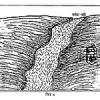लेखक चेतावनी देते हुए कहता है कि जल जो विकास का मूल है, तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। जल के संरक्षण की वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता पर बल देते हुए वह जल के सक्षम उपयोग के लिए सतत शैक्षिक अभियान चलाए जाने की मांग करता है। वह आगे कहता है कि जल संसाधन नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि लोकलुभावन तर्कों पर।
यद्यपि जल इस ग्रह का सर्वाधिक उपलब्ध संसाधन है तथापि मानव उपयोग के लिए यह तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। समस्त जल संसाधन का 97.4 प्रतिशत भाग खारे पानी का है; 1.8 प्रतिशत बर्फ के रूप में है और केवल 0.8 प्रतिशत भाग ही मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है और यही जीवन, विकास और पर्यावरण को कायम रखे हुए है। इस अनन्त और (किन्तु) भंगुर संसाधन का अविवेकपूर्ण एवं अन्धाधुंध उपयोग जल उपलब्धता की समस्या को और सघन बना देता है। मानव मात्र के लिए यह शुभ सूचक नहीं है। संक्षेप में महत्त्वपूर्ण विकास प्रक्रिया संकट में पड़ गई है।
आसन जल संकट पर एक संक्षिप्त चेतावनी जनवरी, 1992 में आयरलैण्ड की राजधानी डबलिन में ‘जल एवं पर्यावरण’ विषय पर हुए अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई थी। इसमें कहा गया था: ‘‘मीठे पानी की कमी और दुरुपयोग ने निरन्तर विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक गम्भीर और लगातार बढ़ता खतरा पैदा कर दिया है। मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास और वह पर्यावरण प्रणाली जिस पर यह सब निर्भर है, सभी खतरे में पड़ जाएँगे यदि जल एवं भूमि संसाधनों का वर्तमान दशक में अधिक कारगर ढँग से प्रबन्ध नहीं किया गया।’’
डबलिन वक्तव्य में आगे कहा गया: ‘‘ये समस्याएँ काल्पनिक नहीं हैं और न ही हमारे ग्रह को सुदूर भविष्य में प्रभावित करने वाली हैं वे अब भी विद्यमान हैं और मानव समाज को इस समय भी प्रभावित कर रही हैं। लाखों-करोड़ों लोगों के भावी अस्तित्व के लिए इस समस्या का समाधान तत्काल और प्रभावी कार्यवाही द्वारा किए जाने की आवश्यकता है’’।
इस वक्तव्य में की गई टिप्पणी अन्य अनेक देशों की अपेक्षा भारत पर अधिक लागू होती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत उन कुछ चुने हुए देशों में से है जहाँ प्रकृति ने असीम जल सम्पदा दी है और यदि उसका बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाए तो वह हमारी आवश्यकता से अधिक ही होगी। परन्तु इन संसाधनों का भौगोलिक वितरण कुछ टेढ़ा है। देश के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग के लायक जल भी नहीं है जबकि कुछ क्षेत्र जहाँ यह संसाधन बहुतायत में है, पर्यावरण की परवाह किए बिना अविवेकपूर्ण ढँग से इसका उपयोग कर रहे हैं। विकास प्रक्रिया और कृषि सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तार ने पानी की माँग को और गहरा दिया है। इस कारण न केवल इसका इस तरह उपयोग करने की आवश्यकता है जिससे यह निरन्तर मिलता रहे बल्कि इसका वैज्ञानिक ढँग से संरक्षण करना भी जरूरी है।
राष्ट्रीय जल नीति
1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति की संस्तुति है कि आर्थिक विकास और कृषि, औद्योगिक तथा शहरी विकास जैसी गतिविधियों की योजनाएँ देश में उपलब्ध जल के दबावों को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जानी चाहिए। देश को उपलब्ध जल के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और आर्थिक गतिविधियाँ तद्नुरूप ही निर्देशित और संचालित की जानी चाहिए।
इस व्यापक सिद्धान्त को अमल में लाने के लिए नीति विषयक दस्तावेज का सुझाव है कि विविध प्रयोजनों के लिए जल का सुचारू ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, कार्यकुशलता सुधारी जानी चाहिए तथा दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के प्रति जागरुकता विकसित की जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि लोगों में शिक्षा, नियमन, प्रोत्साहन और हतोत्साहन के जरिए संरक्षण चेतना बढ़ाई जानी चाहिए।
जल के सबसे बड़े उपभोक्ता के नाते कृषि क्षेत्र को इस बात से अवगत कराना होगा कि वह जल को एक दुर्लभ संसाधन मानकर उसका उचित उपयोग करे, और उन क्षेत्रों में भी जहाँ वह अभी दुर्लभ नहीं हुआ है। क्योंकि जल एक ऐसा संसाधन है जिसका संरक्षण जनांदोलनों के माध्यम से सामूहिक प्रयासों से ही हो सकता है। फसल उत्पादन में जल का कुशल उपयोग का निश्चय ही एक अन्तर्विधायी विषय है और इसके लिए इंजीनियरों, कृषि वैज्ञानिकों, समाज विज्ञानियों और कृषकों का योगदान आवश्यक होगा।
केन्द्रीय जल आयोग के एक आँकलन के अनुसार सतही जल स्रोतों से प्राप्त प्रयोज्य जल की कुल मात्रा लगभग 690 घन किलोमीटर है। इसके अलावा केन्द्रीय भूजल मंडल ने अनुमान लगाया है कि फिर से भरने योग्य (रिचार्जेबल) भूजल की क्षमता 452 घन किलोमीटर की है; जिसे मिलाकर कुल उपलब्ध जल की मात्रा 1142 घन किलोमीटर हो जाती है। इसमें से खेती के लिए अनुमानतः 460 घन किलोमीटर जल का उपयोग होता है। इसमें से 300 घन किलोमीटर सतही जल और 160 घन किलोमीटर भूजल है।
वर्षा जल एकमात्र स्रोत है जिससे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए जल क्षेत्र को दोबारा भरा जा सकता है। देश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सें.मी. मानी जाए तो कुल वृष्टिपात 37 खरब घन मीटर प्रतिवर्ष होता है। इसका लगभग 80 प्रतिशत अंश दक्षिण-पश्चिम मानसून के खाते में जाता है जो चार माह की अल्पावधि में ही इतना जल दे देता है। केन्द्रीय जल आयोग ने अनुमान लगाया है कि कुल वार्षिक वृष्टिपात में से लगभग 8 खरब घन मीटर वर्षा जल भूमि में समा जाता है; करीब 17 खरब घन मीटर जल नदियों में बहते हुए सतही जल के रूप में उपलब्ध होता है और शेष भाप बनकर वातावरण में वापस मिल जाता है।
प्राकृतिक रूप से रिसकर मिट्टी में समा जाने वाला जल तो अवमृदा (जमीन की निचली परत) में स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है और भूजल के रूप में उपलब्ध रहता है, परन्तु वर्षा जल का वह अंश जो भाप बन उड़ जाता है और जमीन पर या नदियों में बहता हुआ समुद्र में जाकर बेकार हो जाता है, कृत्रिम साधनों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। दरअसल यही वह सम्भावना है जिसका पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लाभकर तरीके से दोहन करने की आवश्यकता है।
उपलब्धता संवर्धन
वर्षा के जल को एकत्र करने के सिद्धान्त पर आधारित जल संरक्षण की प्राचीनतम विधि तालाबों के निर्माण की थी जिससे क्षेत्र विशेष में बहने वाले जल को एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाता था। यह प्राचीन प्रणाली फसलों की सिंचाई और मानव समुदाय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में आज भी खरी उतरी है। तालाब प्रणाली देश के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों जैसे पश्चिमी और मध्य भारत में काफी लोकप्रिय रही है। राजस्थान, मालवा के पठारी क्षेत्रों और समस्त दक्षिण भारत में तालाब प्रणाली फैली हुई है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्राचीन साहित्य इस बात का गवाह है कि उस समय इन संरचनाओं को समाज की सम्पत्ति के रूप में सम्मान दिया जाता था। राजाओं, जमींदारों, गाँवों के सरदारों तथा समाज द्वारा इनका प्रबन्ध कुशलतापूर्वक किया जाता था।
यह स्थिति अंग्रेजों के आने के बाद बदलने लगी। ब्रिटिश कानूनों में जल को व्यक्तिगत अथवा राज्य के स्वामित्व वाला संसाधन माना जाता था और उससे व्यावसायिक लाभ उठाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राजनीतिक और प्रशासकीय कारण भी थे जिनकी वजह से वर्षा जल के संग्रह की इस पारम्परिक और श्रेष्ठ प्रणाली का धीरे-धीरे क्षरण होता गया। अनेक तालाब ऐसे हैं जिन्होंने सदियों तक समाज की सेवा की है परन्तु पिछले 200 वर्षों में उपेक्षा के कारण वे हमारे उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं। इनकी पुरानी प्रतिष्ठा लौटाना एक दुश्वार कार्य है क्योंकि इसमें काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। अनेक राज्यों में इस उद्देश्य से व्यापक योजनाएँ बनाई गई हैं जिन पर सही तरीके से अमल की आवश्यकता है।
पिछली दो शताब्दियों में सिंचाई के लिए जल के उपयोग के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया। छोटे-छोटे तालाबों की अपेक्षा बाँध बनाकर बड़े जलाशयों में पानी रोका जाने लगा और नहरों का जाल बिछाकर खेतों और अन्य उपभोक्ताओं तक पानी पहुँचाया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इस संकल्पना को बहुउद्देशीय सिंचाई एवं पनबिजली परियोजनाओं के जरिए एक विस्तृत जल संसाधन विकास नीति में संशोधित कर दिया गया।
आधुनिक तकनीक
 सतह जल के भंडारण और वाहक प्रणाली के विस्तार के फलस्वरूप अनेकों समस्याओं ने जन्म लिया है। इसमें सबसे उल्लेखनीय जलाक्रान्ति की समस्या है जो समुचित और विस्तृत निकासी व्यवस्था की कमी के कारण पैदा होती है। आसानी से उपलब्ध पानी के कृषि कार्य में अत्यधिक उपयोग से यह समस्या और भी विकट हो गई है। इसके कारण अनेक ऐसे उर्वरा क्षेत्र अनुर्वर हो गये हैं जो इससे पहले वैसे नहीं थे।
सतह जल के भंडारण और वाहक प्रणाली के विस्तार के फलस्वरूप अनेकों समस्याओं ने जन्म लिया है। इसमें सबसे उल्लेखनीय जलाक्रान्ति की समस्या है जो समुचित और विस्तृत निकासी व्यवस्था की कमी के कारण पैदा होती है। आसानी से उपलब्ध पानी के कृषि कार्य में अत्यधिक उपयोग से यह समस्या और भी विकट हो गई है। इसके कारण अनेक ऐसे उर्वरा क्षेत्र अनुर्वर हो गये हैं जो इससे पहले वैसे नहीं थे। वाहक व्यवस्था से होने वाले ह्रास, सतह जल के अनुचित वितरण और उसके अत्यधिक उपयोग से जलाक्रान्ति, और मृदा की लवणता के अनुभव के बाद मृदा एवं जल संरक्षण की तकनीक के ज्ञान में पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फिर भी इस ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। इसलिए अब जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों सहित उन्नत जल प्रौद्योगिकी वाले पैकेज के जरिए सिंचाई जल के वैज्ञानिक प्रबन्धन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
सतह जल प्रणाली के विस्तार के साथ-साथ कुएँ खोद कर भूजल का दोहन भी स्वतंत्रता के बाद के काल में तेजी से बढ़ा। नहर प्रणालियों वाले क्षेत्रों में खोदे गए कुँओं और नलकूपों के विस्तार से भूजल के सतह को ऊपर उठने से रोकने में काफी सहायता मिली। इसके फलस्वरूप जलाक्रान्ति (वाटर लॉगिंग) और उसके कारण होने वाली मृदा लवणता में वृद्धि और भू-क्षरण की समस्याओं का भी रोकने में सफलता मिली। परन्तु कुछ क्षेत्रों में यह घातक भी सिद्ध हुई है। जल व्यवस्था को सबसे अधिक हानि उन क्षेत्रों में भूजल के दोहन से हुई है जहाँ वर्षा से होने वाली वार्षिक भराई (रिचार्जिंग) उसकी निकासी (उपयोग) से कम है। इसने कुल पारिस्थितिकी को ही विचलित कर दिया है।
यद्यपि देश के अनेक क्षेत्रों में भूजल के क्षीण होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, परन्तु इसकी सीमा का ठोस आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों को गहरे (डार्क), धुँधले (ग्रे) और उजले (व्हाइट) वर्गों में विभाजित करने की वर्तमान पद्धति से क्षीणता का केवल मोटा-मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये श्रेणियाँ मुख्य रूप से वर्षा जल की प्राप्ति (रिचार्ज) के मुकाबले इस्तेमाल की मात्रा के अनुपात पर आधारित हैं। 85 प्रतिशत या अधिक की दर से उपयोग में आने वाले क्षेत्र को ‘गहरा’ कहा जाता है, 65 से 85 प्रतिशत वाले क्षेत्र को ‘धुंधला’ और अन्य क्षेत्रों को ‘उजला’ कहा जाता है।
भूजल के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न समस्या की गम्भीरता का सही चित्रण राष्ट्रीय स्तर के औसत आँकड़ों से नहीं किया जा सकता। हालाँकि वर्षा से प्राप्त जल और उसके उपयोग का राष्ट्रीय औसत केवल 30 प्रतिशत ही है, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में स्थिति अधिक गम्भीर है जहाँ इस्तेमाल में लाए जाने वाले वर्षा जल औसत दर 80 से 98 प्रतिशत के बीच रहती है। पंजाब के 6 जिलों (कपूरथला, जालंधर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और अमृतसर) तथा हरियाणा के तीन जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल और महेन्द्रगढ़) में तो वृष्टि जल की तुलना में भूजल के उपभोग की दर 140 प्रतिशत तक पहुँच गई है। कपूरथला में उपभोग की यह दर 259 प्रतिशत तक हो गई है। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में तथा एकाध और स्थानों में भी जल उपभोग की यह दर काफी अधिक है।
इस क्षेत्र की दयनीय स्थिति के पीछे जो कारण हैं उनमें जल के उपयोग और जल पर अधिकार सम्बन्धी पुराने कानून, जल सम्पदा के उपयोग और संरक्षण पर समाज के नियन्त्रण और सामूहिक निर्णय के अधिकार में कमी; जल शुल्क में वृद्धि हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और फसलों के लिए जल उपयोग सुधार के उपायों में असफलता प्रमुख है।
व्यावहारिकता की आवश्यकता
यह एक विडम्बना ही है कि भारत में भूजल पर अधिकार आज भी पिछली शताब्दी में ब्रिटिश सामान्य कानून की तर्ज पर बने कानून से ही निर्देशित होता है। इस पुराने कानून में भू-स्वामी को उसकी जमीन के नीचे के जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन से कितना भी पानी खींच लेने के लिए स्वतंत्र भी है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को संशोधित करने की स्पष्ट आवश्यकता है। समकालीन संवैधानिक मूल्यों और आज की सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए उन नदी तटवर्ती अधिकारों के सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या की भी आवश्यकता है जिनके आधार पर सतह-जल के नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की धारा 21 की पुनर्व्याख्या करते हुए जल के अधिकार को भी जीवन के अधिकार जैसे ही मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर जल कानूनों के मूल बुनियादी सिद्धान्तों को पहले ही एक नया आयाम दे दिया है। इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 39 (ख) (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त) के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे सभी लोग उनका भलीभाँति लाभ उठा सके।
चूँकि अपनी गतिशील प्रकृति के कारण पानी एक साझी सम्पत्ति है, जल सम्बन्धी कानूनों को अभिगमन, न्याय और सामाजिक समानता के सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखना होगा। इन कानूनों को जल संसाधनों की जल विज्ञान सम्बन्धी इकाई को भी मान्यता देनी होगी तथा सतह के और भूमि के नीचे के जल के संयुक्त प्रयोग की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा सतह और भूजल के अधिकारों के प्रशासन को एक साथ मिलाकर किया जा सकता है।
पानी के कुशल और बेहतर उपयोग के लिए कुछ हद तक पानी पर व्यक्तिगत अधिकार होना यद्यपि आवश्यक है परन्तु अधिकतर इन अधिकारों का नतीजा उल्टा ही निकलता है क्योंकि पानी जैसे दुर्लभ स्रोत का उपयोग जिस तरह किया जाता है वह समानता और पारिस्थितिकीय सुरक्षा की वांछित धारणाओं के विपरीत ही होता है। इसलिए अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है जो न केवल सामूहिक जल उपभोग की सीमा पर सामाजिक नियन्त्रण सुनिश्चित करे, वरन विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को जल के आवंटन और वितरण पर भी निगरानी रखे।
तथापि जल का विकास और नियमन चूँकि राज्य का विषय है, जल सम्बन्धी अधिकारों को बदलने में केन्द्र की कोई खास भूमिका नहीं है। वह अधिक से अधिक जो कर सकता है और ऐसा किया भी गया है वह यह कि एक आदर्श विधेयक बनाकर राज्यों को भेजे और उन्हें सुझाव दे कि वे अपने कानूनों को कमोबेश उसी आधार पर तैयार करें। ऐसा एक आदर्श विधेयक बनाकर 1970 में राज्यों को दिया गया था परन्तु उसके बारे में राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही थी। विधेयक में अन्य बातों के अलावा राज्य सरकारों को यह अधिकार देने पर भी विचार किया गया था कि वे व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक तौर पर निर्मित कुँओं, नलकूपों आदि भूजल दोहन की संरचनाओं को सीमित करने की शक्ति हासिल कर सकें। केवल पीने का पानी निकालने की छूट इसमें दी गई थी।
करीब दो दशक बाद केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रालय ने एक बार फिर 1990 में एक विशेषज्ञ समिति गठित कर विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा कराई। इस दल की सिफारिशों के आधार पर तैयार संशोधित विधेयक 1992 में राज्यों को भेजा गया परन्तु इस बार भी राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही।
इसी प्रकार पानी की दरों में वृद्धि की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है परन्तु राज्य सरकारें ऐसा करने का राजनीतिक साहस जुटा नहीं पा रही हैं। वास्तव में कुछ राज्यों ने तो इसका उल्टा ही किया है। पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए दरों में वृद्धि करने के बजाय उन्हें या तो कम कर दिया गया है या बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। लोकप्रियता हासिल करने की यह कोशिश थोड़े समय के लिए तो लाभ दे सकती है परन्तु बाद में इससे अनर्थ ही होता है।
जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय यद्यपि महत्त्वपूर्ण होते हैं लेकिन वे ऐसा करने के एकमात्र उपाय नहीं हैं। अत्यधिक उपभोग को फसल पद्धति के विविधीकरण (अदलबदल कर फसलें लेना), ‘गहरे’ और ‘धुँधले’ क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन सीमित कर तथा स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियाँ अपनाकर भी नियन्त्रित किया जा सकता है।
इसके अलावा भूजल को पुनः आवेशित करने की कृत्रिम विधियों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इससे भूमि के नीचे के प्राकृतिक जलाशय में पानी भरा जा सकता है। इस सन्दर्भ में कहना होगा कि आजकल जल संभर (वाटरशेड) योजनाओं पर जो जोर दिया जा रहा है वह उचित ही है क्योंकि इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु में प्राप्त वर्षा जल को संरक्षित कर बाद में उसे उपयोग योग्य बनाना ही है। इस आशय के लिए अपनाए जाने वाले नागरिक (सिविल) और यांत्रिक उपाय मिट्टी और जल के ह्रास को रोकने में तो सहायक होते हैं उनसे पारिस्थितिकीय सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलता है।