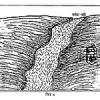Source
जल, जंगल और जमीन - उलट-पुलट पर्यावरण (2013) पुस्तक से साभार
जल संकट में नवीन और प्राचीन की गुंजाईश नहीं होती है। प्रकृति पानी गिराने का तरीका अगर नहीं बदलती है तो संग्रह के तरीके कैसे बदल सकते हैं? पानी रोकने का तरीका फैशन नहीं है, जो हर दो साल में बदला जाये। कुंड, तालाब, नदियों, पोखरों आदि में जल संग्रह होकर भूजल ऊपर उठता है।
विकास के लिये जो पद्धति हमने अपनाई है, उसका कोई भी सम्बन्ध पर्यावरण की गुलामी या आजादी से नहीं है। आजादी से पहले विकास की अवधारणा प्रकृति और संसाधनों के साथ तालमेल बिठाने वाली थी, लेकिन जब हम आजाद हुए, उसके बाद विकास की अवधारणा ज्यादा विकसित हुई है। आजादी के बाद विकास की अवधारणा प्रकृति और संसाधनों का हरसम्भव दोहन करने की हो गई है। देश को जिस दिशा में जाना चाहिए था, उस दिशा में न जाकर वह बिल्कुल विपरीत दिशा में गया है। मोटे तौर पर इस विकास की धारणा के कारण प्राकृतिक विपदाओं का पहाड़ खड़ा हो गया है।आजादी के तुरन्त बाद देश के कर्णधारों के ऊपर बाढ़ वगैरह की समस्या आई, तब उन्होंने एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1954 में बनाया था। ऐसा माना गया था कि देश में अब बाढ़ नहीं आएगी। अगर बाढ़ आएगी तो आयोग इतना सक्षम है कि उस पर नियंत्रण पा लेगा। बहुत अच्छे लोगों के ऊपर इसका जिम्मा था। पानी की तकनीक जानने वाले लोग भी थे और उसकी सामाजिक और राजनीतिक समझ वाले अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता भी थे। उस समय आजादी का उजाला था, इसलिये बेईमानी का प्रतिशत भी बहुत कम था, लेकिन बाढ़ नियंत्रण आयोग ने ज्यों-ज्यों काम करना शुरू किया, उसने विकास के उन्हीं सब कामों को बाढ़ नियंत्रण के साथ जोड़ा, मसलन बड़े-बड़े बाँध बनाना आदि। यह काम अत्यन्त निरापद निकला। आज राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग को 50 साल पूरे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात के हिस्से में आई बाढ़ मधुबन बाँध को खोलने से आई है। पंजाब में आई बाढ़ वहाँ के बाँध में ज्यादा पानी आने और नहरों के टूटने से आई है। यह परिस्थिति आपको बिहार के उन हिस्सों में मिल जाएगी, जहाँ नेपाल पर हम सीधे दोष नहीं मढ़ पा रहे हैं, अन्यथा कह देते कि बाढ़ नेपाल के कारण आई है। नेपाल कहीं नहीं पानी रोकता है। यह सब नए विकास की देन है कि हम कभी बाढ़ और कभी सूखे के कारण डूबते हैं।
बाढ़ का प्रबन्धन नदी-जोड़ो से हो सकता है या नहीं, इसमें सच या झूठ खोजने की जरूरत नहीं है। लोगों में उतावलापन होता है कि हम अपने समय में सब ठीक करके जाएँ, परन्तु प्रकृति का कैलेंडर, हमारे कैलेंडर से मेल नहीं खाता। नदियाँ हजारों-लाखों साल में अपना रास्ता बनाती हैं। उन्हें जब अपने को जोड़ना होता है, वह जोड़ लेती हैं। हम चाहते हैं कि यह काम 5 साल या 20 साल में कर लें। हमारे रहते यह कार्य पूरा हो जाये। हिमालय में गंगा और यमुना को देखें तो उनमें बहुत दूरी नहीं है, परन्तु यह बहुत दूर-दूर चक्कर लगाकर, इलाहाबाद में जाकर अपने को जोड़ लेती हैं। प्रकृति ने धीरे-धीरे दोनों नदियों को जोड़ने की पूर्व तैयारी की होगी। ऊपर की धारा मिलाने से पूर्व नीचे की धारा को मिलाने का सारा इन्तजाम किया होगा। पहले दोनों के लिये भूगोल तैयार किया होगा, तब जाकर दोनों को जोड़ा होगा। फिर बिहार पार करने के बाद वह बंगाल में जाकर समुद्र में मिलने से पहले असंख्य धारों में बन्द हो जाती है। इसलिये नदी को जोड़ने-तोड़ने का काम प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
पानी के बारे में प्रतिव्यक्ति घन मीटर और लीटर की जो पद्धति है, वह योजनाकारों की शब्दावली है। इस पद्धति से उन्होंने देश को ज्यादा पानी उपलब्ध करा दिया हो, ऐसा नहीं है। अन्य मामलों में भारत को गरीब देशों में गिना जाता होगा, लेकिन पानी के मामलों में हमारा देश अमीर है। हमें प्रत्येक समाज के पानी की जरूरत को समझना होगा। चेरापूँजी, गोवा, कोंकण में बहुत पानी गिरता है। वहाँ खेती, घर और जानवरों के लिये पानी का उपयोग अधिक हो सकता है, परन्तु जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाकों में जहाँ पानी बहुत कम गिरता है, जाहिर है कि वहाँ पानी का उपयोग तय किया जाना चाहिए। कहीं पानी बहुत कम है, परन्तु जीवन को चलाने के काम में उसकी सुगन्ध न जाए, इतना ध्यान रखकर समाज ने अपने उपयोग के तौर-तरीके गढ़े होंगे। हालांकि इसे तराजू पर रखकर तय नहीं किया जा सकता, इसे विवेक पर छोड़ना ही ठीक होगा। यह सच है कि हमारे देश में इस कोने से उस कोने तक पानी ठीक मिलता है। हाल के दिनों में पानी की बर्बादी और छीना-झपटी भी हुई है। बहुत सारा पानी चोरी चला गया है। राजनीतिक रूप से बलशाली इलाका कमजोर इलाकों से पानी छीन लेता है। इस कारण से यह समस्या हमारे सामने आई है। हमें घन मीटर और लीटर के चक्कर को छोड़कर क्षेत्र की क्या जरूरत है, इसके आधार पर हल निकालना होगा।
जब हमें आजादी नहीं मिली थी, तब हमारे गाँवों में जल-प्रबन्धन बेहतर था। धीरे-धीरे हमारे गाँवों के जलस्रोत नष्ट होते चले गए हैं। योजना आयोग ने समस्यामूलक गाँवों की एक सूची बनाई थी। आयोग प्रत्येक साल इसका हिसाब-किताब रखता है। आज इन गाँवों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ी है, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि सरकार इस पर बहुत खर्च करती है। क्या सरकार समस्या बढ़ाने पर पैसा खर्च कर रही है? कुछ गाँवों ने सरकार की ओर मुँह न करके अपनी समस्या का हल खुद निकाला है। सरकार अपने बजट का हजारवाँ हिस्सा भी प्रतीक के रूप में उन गाँवों को देती तो सम्बन्धों में सम्मान बढ़ता। यह भावना विकास के आसपास होती। पीने योग्य पानी हर हालत में आम जनता को मिलना ही चाहिए। पीने के पानी पर कितना भी खर्च कर पानी उपलब्ध कराया जाये, यही उचित है। जिन इलाकों में पानी कम गिरता है, वहाँ का भूजल बहुत खारा होता है। इस स्थिति में वर्षाजल पारम्परिक स्रोतों में इकट्ठा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। समाज ने हजारों वर्षों के परिश्रम के बाद जिन परम्पराओं का विकास किया, उनकी हमने उपेक्षा की है। 100-200 कि.मी. पाइप लाइन बिछाकर मीठा जल लाने का झूठा वायदा किया है। यह एक-दो दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला है। हैण्डपम्प और ट्यूबवेल खारा पानी निकालते हैं। कई इलाकों में भेड़-बकरियों ने पानी को पीने से नकार दिया है। ऐसे इलाकों में (बाड़मेर) आधुनिक मित्र संस्था ‘सम्भव’ ने पुरानी परम्परा को सहेजने की कोशिश की, जिसके परिणम अच्छे निकले हैं। योजनाकारों और सरकारों को जाकर उन्हें देखना चाहिए।
जल संकट में नवीन और प्राचीन की गुंजाईश नहीं होती है। प्रकृति पानी गिराने का तरीका अगर नहीं बदलती है तो संग्रह के तरीके कैसे बदल सकते हैं? पानी रोकने का तरीका फैशन नहीं है, जो हर दो साल में बदला जाये। कुंड, तालाब, नदियों, पोखरों आदि में जल संग्रह होकर भूजल ऊपर उठता है। फिर साल भर हम नए-पुराने अलग-अलग तरीकों से पानी को खींचकर उपयोग में लाते हैं। तरुण भारत संघ, सम्भव आदि संस्थाओं और कुछ जगह सरकार (मध्य प्रदेश) ने पुरानी परम्परा को जीवित कर मीठा जल हासिल किया है। आज पर्यावरण की अनगिनत चुनौतियाँ हमारे समक्ष हैं। जल, मिट्टी, हवा, जंगल, बाँध, पहाड़ और शहर सभी के साथ कोई-न-कोई समस्या उभरकर आई है। आधुनिक विकास ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है, जहाँ संकट न हो। एक सन्तुलित व्यवस्था, जिसमें बाधा डालकर कुछ सुविधाएँ देकर, जो असुविधाएँ दी हैं, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है।
जल, जंगल और जमीन - उलट-पुलट पर्यावरण (इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को पढ़ने के लिये कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें) | |
क्रम | अध्याय |
पुस्तक परिचय - जल, जंगल और जमीन - उलट-पुलट पर्यावरण | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |