Source
भारत में वैश्वीकरण प्रभाव और विकल्प, कल्पवृक्ष प्रकाशन, पुणे, 2012
भूमिका
अगर मानव समाज का असली उद्देश्य खुशहाली, आजादी और सम्पन्नता है तो धरती और अपने आप को खतरे में डाले बिना, आधी से ज्यादा मानवता को पीछे छोड़े बिना भी यह उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। यह बात भारत के लिये भी उतनी ही सही है जितनी किसी और देश के लिये सही है हालाँकि अलग-अलग जगह के पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात के हिसाब से विकल्पों में बदलाव आते जाएँगे।
 हमें प्रकृति की अनमोल पर्यावरणीय उपयोगिता का आदर व संरक्षण करना चाहिएइंसानी खुशहाली व सम्पन्नता की वैकल्पिक रूपरेखा को मोटे तौर पर मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र (रेडिकल इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी - रेड) कहा जा सकता है। मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र ऐसी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं का समूह है जो पर्यावरणीय टिकाऊपन और मानव समानता के सिद्धान्तों के आधार पर सभी नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार व अवसर देंगी।
हमें प्रकृति की अनमोल पर्यावरणीय उपयोगिता का आदर व संरक्षण करना चाहिएइंसानी खुशहाली व सम्पन्नता की वैकल्पिक रूपरेखा को मोटे तौर पर मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र (रेडिकल इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी - रेड) कहा जा सकता है। मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र ऐसी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं का समूह है जो पर्यावरणीय टिकाऊपन और मानव समानता के सिद्धान्तों के आधार पर सभी नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार व अवसर देंगी।प्राकृतिक इलाकों और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की सतत एकबद्धता को पर्यावरणीय टिकाऊपन की संज्ञा दी जाती है जिसमें जैवविविधता को बनाए रखना जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार होता है। मानवीय समता वास्तव में अवसरों की समानता, सभी के लिये निर्णयकारी मंचों तक पूरी पहुँच (जिसमें विकेन्द्रीकरण और सहभागिता के सिद्धान्त शामिल हैं), मानव उद्यमों के लाभों के वितरण व प्रयोग में समानता (तमाम वर्गों, जातियों, आयु वर्गों, नस्ल और अन्य भेदों के परे) और सांस्कृतिक सुरक्षा का मिश्रण होती है।
इससे जुड़े कुछ बुनियादी सिद्धान्त या मूल्य ये हैं जिनका हमें सम्मान करना होगा : विविधता और बहुलता (वैश्वीकरण की समरूपवादी प्रवृत्तियों के विपरीत), परस्पर सहयोग और सामुदायिक क्षेत्रों व संसाधनों का साझा प्रबन्धन (गलाकाट प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद के विपरीत), स्पष्ट मानवाधिकार और सभी के लिये पर्यावरणीय दायित्व, श्रम का सम्मान (यानी केवल बौद्धिक कार्य को ही श्रेष्ठतर न माना जाए), सुख की चाह में गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों तरह के साधनों का मिश्रण (खालिस भौतिकवाद के विपरीत), मानव सम्बन्धों तथा टकरावों से निपटने के परम्परागत तरीकों की बहाली, अहिंसा, ‘गहन’ लोकतंत्र जिसमें सभी के पास निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार व क्षमता हो तथा प्रकृति व गैर-मानवीय प्रजातियों के अधिकारों का आदर करना।
उपरोक्त और अन्य सम्भावित सिद्धान्तों को मिलाकर रेड मनुष्यों व मानवता तथा शेष प्रकृति के बीच सतत और परस्पर सम्मानजनक संवाद का दर्शन है। इसे कोई एक रास्ता या ब्लूप्रिंट मानना भूल होगी बल्कि इसमें कई रास्ते शामिल होंगे। इनमें ऐसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं जिनको कभी मूल्यवान माना जाता था लेकिन अब पुरातन और ‘आदिम’ माना जाने लगा है। इनमें आजीविका स्तरीय अर्थव्यवस्थाएँ, चीजों के लेन-देन की व्यवस्था, स्थानीय हाट-बाजार में होने वाले व्यापार, मौखिक ज्ञान, श्रम व मनबहलाव का मिश्रण, मशीन को मालिक की बजाय एक साधन के रूप में देखना, स्थानीय चिकित्सा परम्पराएँ, दस्तकारी, अभिभावकों और बड़े-बुजुर्गों के साथ काम करके सीखना, फिजूलखर्ची को बुरा मानना आदि सिद्धान्त शामिल हैं। इसका मतलब परम्पराओं को आँख मूंदकर मान लेना भी नहीं है। परम्परागत भारत में भी बहुत कुछ ऐसा है (जैसे कि जातिवाद व महिलाओं का शोषण) जिसको हमें अब हमेशा के लिये छोड़ देना चाहिए। वास्तव में मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र अतीत के साथ एक सुचिंतित सम्बन्ध की कल्पना है, ऐसे बहुत सारे मूल्यवान व्यवहारों की खोज का सिलसिला है जिनको अब भुला दिया गया है। ये उस तरह का पुनरुत्थानवाद भी नहीं है जिसकी भारत के दक्षिणपंथी हिन्दू अहमन्यवादी बात करते हैं। हमें परम्पराओं को उन लोगों के चंगुल से बचाना होगा जो उन्हें धर्मान्ध तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्थानीयकरण
स्थानीयकरण का रुझान वैश्वीकरण के विपरीत है। यह धारणा इस विश्वास पर आधारित है कि जो लोग संसाधनों (जंगल, समुद्र, तट, खेत, शहरी सुविधाएँ आदि) के सबसे निकट रहते हैं उनकी ही उन संसाधनों पर सबसे ज्यादा दावेदारी भी होनी चाहिए; उन्हीं के पास उन संसाधनों के प्रबन्धन का सबसे अच्छा ज्ञान होता है। बेशक, हमेशा ऐसा नहीं होता और भारत में बहुत सारे समुदाय सरकार के प्रभुत्व वाली नीतियों के कारण इन संसाधनों के प्रबन्धन की क्षमता गँवा चुके हैं क्योंकि इन नीतियों ने लोगों की अपनी संस्थागत संरचनाओं, परम्परागत कायदे-कानूनों और दूसरी सामर्थ्यों को पंगु बना दिया है। फिर भी, अगर समुदायों को गैर-सरकारी संगठनों और सरकार की तरफ से संवेदनशीलता के साथ मदद मिले तो अनिवार्य उत्पादन, उपभोग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सेवाओं के स्थानीयकरण की तरफ बढ़ा जा सकता है। जल संरक्षण, जैवविविधता संरक्षण, शिक्षा, अभिशासन, खाद्य एवं सामग्री उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, कचरा प्रबन्धन और अन्य क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत स्तर पर भारत में हजारों अभिनव प्रयोग चल रहे हैं। ये प्रयास गाँव और शहर, दोनों जगह देखे जा सकते हैं। (भारतीय संविधान में किए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन (ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के पक्ष में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण) को तार्किक परिणिति तक ले जाया जाए तो वास्तव में इसका आशय स्थानीयकरण से ही है। इसके कुछ सजीव उदाहरण ये हो सकते हैं :
1. डेकन डेवलपमेंट सोसायटी की दलित महिला किसानों, ग्रीन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे समुदायों, बीज बचाओ आन्दोलन से जुड़े किसानों और नवदान्या के जैवपंचायत नेटवर्क ने फसलों की विविधता का रास्ता अपनाकर टिकाऊ खेती का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
2. उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड नागालैंड और अन्य प्रदेशों में जंगलों, तालाबों-नदियों, घास के मैदानों और तटीय/समुद्री क्षेत्रों तथा वन्य जीव आबादियों व प्रजातियों के संरक्षण व प्रजनन/पुनर्जीवन के लिये हजारों समुदाय आधारित प्रयास चल रहे हैं।
3. नागालैंड सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य आयामों के ‘सामुदायीकरण’ (अधिक स्थानीय नियंत्रण) के सफल प्रयोग किए हैं।
4. सैकड़ों गाँव निर्जल, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जल आत्मनिर्भरता का सफल प्रयोग कर चुके हैं। इसके लिये उन्होंने पानी के विकेन्द्रीकृत संरक्षण और उसके प्रयोग के लिये सख्त स्वनियमन का रास्ता अपनाया है। तरुण भारत संघ द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में किया गया ऐसा एक प्रयोग उल्लेखनीय है।
5. अपनी सारी जरूरतों के लिये परजीवियों की तरह गाँवों पर शहरों की निर्भरता के शास्त्रीय मॉडल से दूर जाने का उदाहरण भुज (कच्छ, गुजरात) में देखा जा सकता है। हुनरशाला, सहजीवन, कच्छ महिला विकास संगठन और एसीटी जैसी संस्थाओं ने मिलकर झुग्गीवासियों, महिला मंडलों और अन्य नागरिकों को संगठित करके जलागम क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने और एक विकेन्द्रीकृत जल भंडारण व प्रबन्धन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। ये संगठन ठोस कचरे के निस्तारण, गरीब महिलाओं के लिये रोजगारों, पर्याप्त स्वच्छता और सबके लिये सम्मानजनक आवास सुविधाओं का बन्दोबस्त करते हैं। यहाँ के अलावा बंगलुरु, पुणे व अन्य शहरों में भी बहुत सारे नागरिक विकेन्द्रीकृत, स्थानीय नियोजन के लिये 74वें संविधान संसोधन की मदद ले रहे हैं।
6. स्थानीयकरण की सफलता के लिये ये जरूरी है कि हम जाति व्यवस्था, अन्तर्धार्मिक प्रक्रियाओं और नर-नरी (जेंडर) सम्बन्धों में छिपे सामाजिक-आर्थिक शोषण को भी सम्बोधित करें। इस तरह की असमानताओं को निश्चय ही दूर किया जा सकता है - यह बात आन्ध्र प्रदेश में डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी की गतिविधियों के जरिए दलित महिलाओं को मिल रहे आदर व गौरव, तमिलनाडु के कुथम्बक्कम गाँव में दलितों व ‘ऊँची’ जातियों के बीच पहले से ज्यादा समानता तथा नर्मदा बचाओ आन्दोलन की जीवनशालाओं में आदिवासी बच्चों के सशक्तीकरण के अनुभवों से समझा जा सकता है। वैसे भी, इस आशय के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं है कि वैश्वीकरण ने जाति, धर्म और नर-नारी आधारित शोषण पर कोई उल्लेखनीय अंकुश लगाया है और न ही इस आशय के साक्ष्य उपलब्ध हैं कि इसने नए किस्म की असमानताओं को जन्म नहीं दिया है।
भूक्षेत्र स्तर पर काम करना
स्थानीय और छोटे स्तर पर काम करना ही पर्याप्त नहीं होगा। हम अभी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनमें से बहुत सारी बहुत व्यापक पैमाने की समस्याएँ हैं। ये ऐसी समस्याएँ हैं जो विशाल भू-क्षेत्रों (और समुद्रों), देशों, क्षेत्रों और वस्तुतः पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं। वायुमण्डलीय परिवर्तन, विषैले पदार्थों का फैलाव और रेगिस्तानों का फैलाव इसी तरह के उदाहरण हैं। भूक्षेत्र और सीमापारीय नियोजन व अभिशासन (जिसे ‘जैवक्षेत्रवाद’ या ‘पर्यावरणीय क्षेत्रवाद’ आदि नाम भी दिए गए हैं) जैसी दिलचस्प नई पद्धतियों को कई देशों और क्षेत्रों में आजमाय जा रहा है। अभी भारत में ये कोशिशें अपनी शैशव अवस्था में हैं लेकिन इनमें से कुछ से निश्चय ही हम सबक सीख सकते हैं। राजस्थान में स्थित अरवरी संसद में राज्य के 72 गाँवों के लोग मिलकर 400 किलोमीटर में फैली नदी तलहटी की सार-सम्भाल का जिम्मा उठाए हुए हैं। वे भूमि, कृषि, जल, वन्य जीवन और विकास के लिये समेकित योजनाएँ व कार्यक्रम तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में वाटर यूजर्स एसोसिएशन की एक फेडरेशन को वाघाड़ सिंचाई परियोजना के प्रबन्धन का काम सौंपा गया है। ये पहला उदाहरण है जब कोई सरकारी परियोजना पूरी तरह स्थानीय जनता को सौंप दी गई है।
 इंसानी खुशहाली के लिये प्रकृति व संस्कृति के संबंध बहुत अनिवार्य हैविकेन्द्रीकृत एवं भूक्षेत्र स्तरीय अभिशासन व प्रबन्धन से आगे बढ़ते हुए ये कह जा सकता है कि प्रत्येक जैव क्षेत्र, प्रान्त और देश के लिये भी भूमि प्रयोग की एक तार्किक पद्धति हो सकती है। इस तरह की योजना पर्यावरणीय एवं सामाजिक दृष्टि से देश की सबसे नाजुक या महत्त्वपूर्ण जमीनों को हमेशा के लिये किसी-न-किसी किस्म की संरक्षित श्रेणी में रख देगी (यह पूरी तरह सहभागी योजना होगी और उसमें लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा)। इस तरह की योजना शहरों और कस्बों को भी जल संरक्षण, छतों और खाली प्लॉट्स में खेती, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन आदि के जरिए अधिकतम सम्भव हद तक संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित करेगी और इस तरह गाँवों के साथ उनका सम्बन्ध केवल परजीवी वाला न रहकर परस्पर लाभ का सम्बन्ध बन जाएगा। ग्रामीण समुदायों के संसाधनों का क्या होता है, इसमें उनकी राय जितनी महत्त्वपूर्ण होगी और अपनी जीवन शैली के बारे में शहरवासियों के भीतर जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, परस्पर सहभागिता के सम्बन्ध उतने ही गहरे होंगे।
इंसानी खुशहाली के लिये प्रकृति व संस्कृति के संबंध बहुत अनिवार्य हैविकेन्द्रीकृत एवं भूक्षेत्र स्तरीय अभिशासन व प्रबन्धन से आगे बढ़ते हुए ये कह जा सकता है कि प्रत्येक जैव क्षेत्र, प्रान्त और देश के लिये भी भूमि प्रयोग की एक तार्किक पद्धति हो सकती है। इस तरह की योजना पर्यावरणीय एवं सामाजिक दृष्टि से देश की सबसे नाजुक या महत्त्वपूर्ण जमीनों को हमेशा के लिये किसी-न-किसी किस्म की संरक्षित श्रेणी में रख देगी (यह पूरी तरह सहभागी योजना होगी और उसमें लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा)। इस तरह की योजना शहरों और कस्बों को भी जल संरक्षण, छतों और खाली प्लॉट्स में खेती, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन आदि के जरिए अधिकतम सम्भव हद तक संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित करेगी और इस तरह गाँवों के साथ उनका सम्बन्ध केवल परजीवी वाला न रहकर परस्पर लाभ का सम्बन्ध बन जाएगा। ग्रामीण समुदायों के संसाधनों का क्या होता है, इसमें उनकी राय जितनी महत्त्वपूर्ण होगी और अपनी जीवन शैली के बारे में शहरवासियों के भीतर जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, परस्पर सहभागिता के सम्बन्ध उतने ही गहरे होंगे।कुल मिलाकर, जैसे-जैसे स्थानीय स्तर पर अनुकूल प्रयासों के जरिए गाँव पुनर्जीवित होते जाएँगे, वैसे-वैसे गाँवों से शहरों की तरफ पलायन भी धीमा हो जाएगा और सम्भव है कि इसकी दिशा उलट जाए। महाराष्ट्र के रालेगाँव सिद्धी और हीवरे बाजार में तथा मध्य प्रदेश के देवास जिले में ऐसा हो चुका है। देवास में समाज प्रगति सहयोग नामक संस्था यही काम कर रही है। झारखंड में जहाँ झाक्राफ्ट संस्था सक्रिय है वहाँ भी कई गाँवों में यह स्थिति बनी है।
स्थानीय से राष्ट्रीय अभिशासन की ओर
मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र की धारणा में लोकतांत्रिक अभिशासन की प्रक्रिया सबसे लघु, सबसे स्थानीय इकाई से शुरू होती है। भारत के संविधान में गाँव और ग्राम समूहों के स्तर पर तथा शहरों में वार्ड समितियों के स्तर पर पंचायतों के जरिए अभिशासन की व्यवस्था की गई है। परन्तु ये प्रतिनिधिक निकाय भी उन्हीं खामियों से ग्रस्त है जिनसे ऊपरी स्तर का प्रतिनिधिक लोकतंत्र ग्रस्त है। इनसे बचने के लिये हमें ग्रामसभा और शहरों में क्षेत्र सभा (वार्ड्स के भीतर लघुतर इकाइयाँ) का सशक्तिकरण करना होगा ताकि किसी टोले/गाँव अथवा शहरी बस्ती के सभी वयस्क निर्णय प्रक्रिया में सहज ढंग से हिस्सा ले सकें। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण फैसले इसी स्तर पर लिये जाने चाहिए और इस बात का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं व अन्य वंचित तबकों की भी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
इसके उदाहरण पहले ही हमारे सामने मौजूद हैं :
1. मेंढा-लेखा (महाराष्ट्र) के गोंड आदिवासी गाँवों ने ‘मुम्बई दिल्ली में हमारी सरकार, अपने गाँव में हम सरकार’ का सिद्धान्त अपनाया है। इस गाँव में सारे फैसले गाँव की पूरी सभा के सामने गाँव के ही अन्य अभ्यास गुट के आधार पर जुटाई गई जानकारियों सहारे सबकी सहमति से लिये जाते हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान भोजन, पानी, ऊर्जा और स्थानीय आजीविका सम्बन्धी सारी बुनियादी जरूरतों को यह गाँव खुद पूरा करने के सफल प्रयास में लगा है। इस गाँव के लोगों ने 1800 हेक्टेयर वन भूमि का भी संरक्षण करके दिखा दिया है जिस पर अब उनको पूरा कानूनी अधिकार भी मिल गया है।
 उत्तर कन्नड़ में घरेलू बगीचों को पुनर्जीवित करने में पथप्रदर्शक भूमिका निभाने वाली स्वर्गीय सावित्री अम्मा
2. उपरोक्त ग्रामीण उदाहरणों के अलावा कुछ शहर भी सहभागी बजटिंग की दिशा में बढ़ने लगे हैं जहाँ नागरिक ही सरकारी बजट को प्रभावित करने के लिये व्यय सम्बन्धी प्राथमिकताएँ शासन के पास भेजते हैं।
उत्तर कन्नड़ में घरेलू बगीचों को पुनर्जीवित करने में पथप्रदर्शक भूमिका निभाने वाली स्वर्गीय सावित्री अम्मा
2. उपरोक्त ग्रामीण उदाहरणों के अलावा कुछ शहर भी सहभागी बजटिंग की दिशा में बढ़ने लगे हैं जहाँ नागरिक ही सरकारी बजट को प्रभावित करने के लिये व्यय सम्बन्धी प्राथमिकताएँ शासन के पास भेजते हैं।बड़े स्तर की अभिशासन संरचनाएँ मूलतः इन्हीं बुनियादी इकाइयों से विकसित होनी चाहिए। इनमें समान पर्यावरणीय विशिष्टताओं वाले ग्राम समूह या ग्राम संघ, भूक्षेत्र स्तरीय संस्थान और ऐसी अन्य संस्थाएँ बनाई जा सकती हैं जो किसी-न-किसी रूप में जिले और राज्य की मौजूदा प्रशासकीय व राजनीतिक इकाइयों से भी सम्बद्ध हों। राज्यों और देशों का अभिशासन एक ज्यादा बड़ी चुनौती जरूर है लेकिन विफल हो चुके या आंशिक रूप से सफल नदी-तलहटी प्राधिकरणों जैसे प्रयोगों से बहुत सारे सबक सीखे जा सकते हैं।
सार्थक शिक्षा एवं स्वास्थ्य
मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र के लिये सबसे प्रासंगिक ज्ञान वह होगा जो पश्चिमी ढंग की शिक्षा तथा उसके फलस्वरूप ‘भौतिक’, ‘प्राकृतिक’ एवं ‘सामाजिक’ विज्ञानों के बीच और इन विज्ञानों तथा ‘कलाओं’ के बीच पैदा कर दी गई कृत्रिम सीमाओं को खारिज करता है। पर्यावरणीय या मानव समाज की प्रणालियाँ इस तरह के साफ-सुथरे बक्सों से नहीं बनती। भूक्षेत्र में जंगल और रिहाइश के बीच, प्राकृतिक और इंसानी परिधि के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। ज्ञान को समावेशी ढंग से सीखने, सिखाने और उसका संचार करने में हम जितना ज्यादा योगदान देंगे, जितना हम विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों को भी सम्मान देंगे, उतना ही ज्यादा हम प्रकृति और उसमें अपने स्थान को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएँगे। बहुत सारे वैकल्पिक शिक्षा एवं सीख के प्रयोग इसी दिशा में बढ़ रहे हैं : आन्ध्र प्रदेश में सक्रिय डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी के पाचासाले जैसे स्कूल और नर्मदा घाटी व उसके निवासियों को महाकाय बाँधों से बचाने के लिये जूझ रहे नर्मदा बचाओ आन्दोलन के जीवनशाला स्कूल, तेजगढ़, गुजरात स्थित आदिवासी अकादमी जैसे कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड स्थित बीज विद्यापीठ व उदयपुर के स्वराज विश्वविद्यालय जैसे मुक्त शिक्षा संस्थान आदि इसी तरह के उदाहरण हैं।
इसी प्रकार कई संगठन लोक स्वास्थ्य प्रणालियों पर भी काम कर रहे हैं। वे समुदायों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के लिये उनका सशक्तिकरण करते हैं। वे परम्परागत और आधुनिक व्यवस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़कर और सुरक्षित भोजन व पानी, पोषण, रोधक स्वास्थ्य उपायों और उपचारक कार्यक्रमों को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास कर रहे हैं।
रोजगार और आजीविका
स्थानीयकरण और भूक्षेत्र नियोजन का मिश्रण आजीविका अवसरों की भी जबर्दस्त सम्भावनाएँ पैदा करता है। इस प्रकार, यह पद्धति भारत की एक बहुत बड़ी समस्या यानी बेरोजगारी को दूर करने का भी साधन बन सकती है। भूमि एवं जल पुनर्नवीकरण तथा इसके फलस्वरूप उपज में इजाफे से रोजगार के विशाल स्रोत पैदा हो सकते हैं और टिकाऊ आजीविकाओं के लिये स्थायी सम्पदाएँ रची जा सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को पर्यावरण-रोजगार के इस समन्वय की दिशा में मोड़ा जा सकता है। नई ‘ग्रीन जॉब’ डील में श्रम-सघन ग्रामीण उद्योगों व बुनियादी ढाँचे, हथकरघे और दस्तकारी, स्थानीय ऊर्जा परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों और ऐसे दूसरे विकल्पों पर भी नए सिरे से जोर देना होगा जिनको लोग अपने नियंत्रण में रख सकें, जिन्हें वे अपने परम्परागत ज्ञान या आसानी से सीखे जा सकने वाले नए कौशलों के सहारे लोग खुद चला सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि मानवोचित श्रम के रूप में परिभाषित ऐसे ‘हरित रोजगारों’ में आजीविका के भारी अवसर हैं जो मौजूदा पर्यावरणीय संकट से निपटने में मदद देंगे। उदाहरण के लिये, जैविक, छोटे पैमाने की खेती परम्परागत रसायन आधारित खेती के मुकाबले ज्यादा लोगों को काम दे सकती है। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा कुशलता जो अभी अपने शैशव चरण में है, वह लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। खेती और ऊर्जा (उत्पादन व कुशलता) तथा परिवहन, ऊर्जा कुशल निर्माण, विकेन्द्रीकृत उद्योग, रीसाइक्लिंग (इस्तेमाल हो चुकी चीजों को फिर से इस्तेमाल योग्य वस्तुओं में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया), वानिकी व अन्य कई क्षेत्रों में भी हमारे सामने अभूतपूर्व सम्भावनाएँ मौजूद हैं। फिर भी, इस सम्भावना का आकलन करने के लिये अभी तक कोई समग्र अध्ययन नहीं किया गया है।
आर्थिक लोकतंत्र
मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र के लिये हमें न केवल राजनीतिक अभिशासन में बल्कि उत्पादन व उपभोग के आर्थिक सम्बन्धों में भी आमूल बदलाव लाने होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ उपभोग का लोकतांत्रीकरण तो करती हैं लेकिन उत्पादन का लोकतांत्रीकरण नहीं करती (वैसे तो ये भी सिर्फ कहने वाली ही बात है कि उपभोक्ता ही ‘परमेश्वर’ है क्योंकि बहुधा उपभोक्ताओं के सामने चुनाव का सिर्फ एक भ्रम मात्र रहता है)। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब विकेन्द्रीकृत उत्पादन सुनिश्चित किया जाए जो उपभोक्ताओं व उत्पादकों के नियंत्रण में हो।
गाँव आधारित या कुटीर उद्योगों, लघु एवं विकेन्द्रीकृत उद्योगों का गांधीवादी प्रस्ताव दशकों से हमारे सामने रहा है। इस तरह का उद्योग सबसे पहले और सर्वोपरि स्थानीय आवश्यकताओं और उसके पश्चात राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर केन्द्रित होगा। यह एक स्थानीय अर्थव्यवस्था का अंग होगा जिसमें उत्पादक-उपभोक्ता सम्बन्ध मुख्य रूप से स्थानीय होंगे इसलिये उस तरह के उत्पादन तथा मौजूदा पूँजीवादी उत्पादन के बीच सबसे बुनियादी फर्क ये होगा कि वह अपने तथा औरों के लिये होगा, मूल रूप से लाभ के लिये नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में होगा।
इस तरह के आर्थिक लोकतंत्र में ग्राम समूह या गाँवों व शहरों के समूह प्रारम्भिक इकाई होंगे। उदाहरण के लिये :
1. तमिलनाडु में कुथम्बक्कम गाँव के सरपंच रामास्वामी इलेंगो 7-8 गाँवों को मिलाकर एक ‘मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ‘मुक्त व्यापार क्षेत्र’ में ये गाँव एक-दूसरे के साथ वस्तुओं व सेवाओं का (परस्पर लाभ के लिये) व्यापार करेंगे जिससे बाहरी व्यापार और शासन पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सके। इस तरह, इन गाँवों का पैसा स्थानीय विकास में पुनः निवेश के लिये इन्हीं गाँवों में रहेगा और उनके आपसी सम्बन्ध भी मजबूत होंगे।
2. गुजरात में भाषा नामक संगठन दर्जनों जनजातीय गाँवों को लेकर एक हरित आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिये प्रयास कर रहा है। यह हरित आर्थिक क्षेत्र टिकाऊपन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता की अवधारणाओं तथा लोगों की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान की भावना पर आधारित होगा।
3. मध्य प्रदेश में नोगाँग कृषि उत्पादक कम्पनी लिमिटेड (एनएपीसीएल) तथा तमिलनाडु में आहारम परम्परागत फसल उत्पादक कम्पनी (एटीसीपीसी) किसानों द्वारा चलाई जा रही ऐसी कम्पनियाँ हैं जो उत्पादकों को सीधे अपने बाजार से जोड़ती हैं।
पैसा तो विनिमय का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा लेकिन यह अज्ञात अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की बजाय स्थानीय नियंत्रण व प्रबन्धन के भीतर होगा और आपस में जुड़े वित्तीय बाजारों के जरिए काम करने वाली वैश्विक पूँजी की अमूर्त शक्तियाँ इसको नियंत्रित नहीं कर पाएँगी। काफी सारा स्थानीय व्यापार स्थानीय मुद्राओं या वस्तु-विनिमय की व्यवस्था के तहत होने लगेगा और भले ही उत्पादों व सेवाओं का मूल्य पैसे में व्यक्त होता रहे, वह एक निर्वैयक्तिक, नियंत्रणमुक्त बाहरी बाजार की बजाय स्वयं देने और लेने वालों के द्वारा निर्धारित होगा। दुनिया भर में न केवल असंख्य प्रकार की स्थानीय मुद्राएँ मौजूद हैं बल्कि व्यापार व सेवाओं के आदान-प्रदान के गैर-मौद्रिक तरीके भी मौजूद हैं।
वित्तीय प्रबन्धन का भी गहरे तौर पर विकेन्द्रीकरण करना होगा। इसे आज के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के महासंकेन्द्रण से मुक्त कराना होगा। वैश्विक संस्थानों और उनकी सट्टेबाजी प्रवृत्तियों को मिली खुली छूट ही ताजा आर्थिक संकट की जड़ है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया भर में पिछले कुछ दशकों के दौरान असंख्य स्थानीय, समुदाय आधारित बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्थाएँ भी पैदा हुई हैं।
सरकार की भूमिका
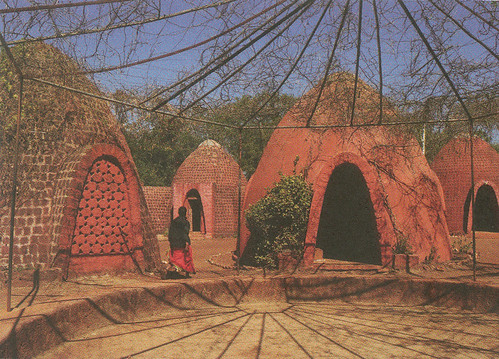 पाचासाले, डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी का वैकल्पिक स्कूल
इन वैकल्पिक भविष्यों का का मूल आधार तो समुदाय (ग्रामीण और शहरी) ही होंगे लेकिन सरकार को कमजोर (मानवीय और गैर-मानवीय, दोनों) तबकों के हित में अपनी कल्याणकारी भूमिका को बरकरार रखना होगा या और बढ़ाना होगा, कम-से-कम कुछ समय के लिये। सरकार समुदायों को उन परिस्थितियों में सहायता देगी जहाँ स्थानीय क्षमता कम है, जैसे संसाधन जुटाने में, अधिकार प्रदान करने में और स्वामित्व सुरक्षा सुनिश्चित करने में। सरकार ऐसे व्यावसायिक तत्वों या अन्य स्वार्थों पर अंकुश लगाएगी जो पर्यावरण या लोगों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। उसे संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को मिले विभिन्न मूल अधिकारों के रक्षक की भूमिका अपनानी होगी और इसके लिये सूचना अधिकार कानून जैसे उचित नीतिगत उपाय भी करने होंगे। और अन्त में, उसे समाजों और राष्ट्रों के व्यापक वैश्विक सम्बन्धों में अपनी भूमिका भी कायम रखनी होगी (जब तक राष्ट्र रहेंगे)।
पाचासाले, डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी का वैकल्पिक स्कूल
इन वैकल्पिक भविष्यों का का मूल आधार तो समुदाय (ग्रामीण और शहरी) ही होंगे लेकिन सरकार को कमजोर (मानवीय और गैर-मानवीय, दोनों) तबकों के हित में अपनी कल्याणकारी भूमिका को बरकरार रखना होगा या और बढ़ाना होगा, कम-से-कम कुछ समय के लिये। सरकार समुदायों को उन परिस्थितियों में सहायता देगी जहाँ स्थानीय क्षमता कम है, जैसे संसाधन जुटाने में, अधिकार प्रदान करने में और स्वामित्व सुरक्षा सुनिश्चित करने में। सरकार ऐसे व्यावसायिक तत्वों या अन्य स्वार्थों पर अंकुश लगाएगी जो पर्यावरण या लोगों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। उसे संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को मिले विभिन्न मूल अधिकारों के रक्षक की भूमिका अपनानी होगी और इसके लिये सूचना अधिकार कानून जैसे उचित नीतिगत उपाय भी करने होंगे। और अन्त में, उसे समाजों और राष्ट्रों के व्यापक वैश्विक सम्बन्धों में अपनी भूमिका भी कायम रखनी होगी (जब तक राष्ट्र रहेंगे)।वैश्विक सम्बन्ध
आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के उलटने का मतलब वैश्विक सम्बन्धों की समाप्ति नहीं है! विचारों, व्यक्तियों, सेवाओं और वस्तुओं का दुनिया भर में प्रवाह हमेशा जारी रहा है और इसने अक्सर मानव समाजों को समृद्धि दी है। वित्त और पूँजी की बजाय स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और सामुदायिक जीवन शैलियों को केन्द्र में लेकर चलने वाली मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र की अवधारणा वास्तव में वैश्विक स्तर पर विचारों व अभिनव प्रयोगों के प्रवाह को ज्यादा सार्थक बनाएगी।
 नर्मदा बांध प्रभावित लोगों की रैली, बड़वानी, मध्य प्रदेशभारत को साझा पर्यावरणीय, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ भी बेहतर सम्बन्ध बनाने होंगे। सीमापारीय भूक्षेत्र व समुद्र-क्षेत्र प्रबन्धन इसका एक उदाहरण है। जिन क्षेत्रों में अभी बहुत तीखा टकराव है (जैसे, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सियाचिन ग्लेशियर) वहाँ संसाधनों के संरक्षण के लिये ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाए जा सकते हैं। वैश्विक धरातल पर शान्ति, अधिकारों और पर्यावरण के सवालों पर विभिन्न सन्धियों को मजबूती देना एक मुख्य कदम होना चाहिए।
नर्मदा बांध प्रभावित लोगों की रैली, बड़वानी, मध्य प्रदेशभारत को साझा पर्यावरणीय, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ भी बेहतर सम्बन्ध बनाने होंगे। सीमापारीय भूक्षेत्र व समुद्र-क्षेत्र प्रबन्धन इसका एक उदाहरण है। जिन क्षेत्रों में अभी बहुत तीखा टकराव है (जैसे, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सियाचिन ग्लेशियर) वहाँ संसाधनों के संरक्षण के लिये ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाए जा सकते हैं। वैश्विक धरातल पर शान्ति, अधिकारों और पर्यावरण के सवालों पर विभिन्न सन्धियों को मजबूती देना एक मुख्य कदम होना चाहिए।क्या इस तरह का रूपान्तरण सम्भव है?
मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र के फलस्वरूप अभिशासन में भारी बदलाव आएँगे और आज के राजनीतिक व व्यावसायिक सत्ता केन्द्र इसका विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सरे लक्षण गिनाए जा सकते हैं जिनको देखकर लगता है कि अगले कुछ दशकों के दौरान ऐसा रूपान्तरण लाया जा सकता है :
1. आर्थिक विकास के स्थापित मॉडल के विभिन्न आयामों के विरुद्ध गैर-सरकारी संगठनों की गोलबन्दी बढ़ती जा रही है। विनाशकारी विकास परियोजनाओं के खिलाफ चल रहे जनान्दोलनों, खासतौर से विस्थापन अथवा पर्यावरण विनाश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलनों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इन्हें शहरी इलाकों में सक्रिय नागर समाज संगठनों से भी मदद मिल रही है।
2. गैर-सरकारी समाज मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद देगा : बहुत सारे मोर्चों पर सरकार की बार-बार विफलताओं से समुदाय आधारित संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों को बुनियादी सुविधाओं व सहूलियतों का जिम्मा लेने और स्थानीय सशक्तिकरण में योगदान देने का मौका मिला है जिसे इस लेख में आए उदाहरणों से समझा जा सकता है।
3. नीतिगत बदलाव व सुधार : गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई एडवोकेसी और स्वयं राज्य तंत्र में मौजूद प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा की गई गतिविधियों से नीतियों में ऐसे कई बदलाव और सुधार आए हैं जो आर्थिक उदारीकरण के सामान्य रुझान के विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। सूचना अधिकार कानून 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2006 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 इस तरह के तीन महत्त्वपूर्ण ताजा उदाहरण हैं। इन तीनों की शुरुआत लोगों की पहलकदमियों से हुई है। आरटीआई कानून राजस्थान, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) जैसे संगठनों के नेतृत्व में रोजगार व परियोजनाओं के सरकारी रिकॉर्ड हासिल करने के लिये चलाए गए स्थानीय संघर्षों से पैदा हुआ था।
4. प्रौद्योगिकीय परिवर्तन : बहुत सारे तकनीकी आविष्कार न केवल मानव जीवन को आसान बन रहे हैं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिये भी संवेदनशील हैं। औद्योगिक व कृषि उत्पादन, ऊर्जा, आवास व निर्माण, परिवहन, घरेलू उपकरण आदि बहुत सारी तकनीकियाँ पहले से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल हैं। बहुत सारी परम्परागत प्रौद्योगिकियों को बहाल करने या जारी रखने के पक्ष में भी एक जनमत बनता जा रहा है। उदाहरण के लिये कृषि, कपड़ा एवं अन्य मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों आदि मे लोग परम्परागत पद्धतियों के महत्त्व पर जोर देने लगे हैं। ‘विकासशील’ देशों के पास बेहद अपव्ययी औद्योगिक ऊर्जा एवं परिवहन प्रौद्योगिकियों से सीधे सुपरकुशल प्रौद्योगिकियों के युग में छलांग लगाने का एक अभूतपूर्व अवसर है - बशर्ते औद्योगिक देश उन्हें ऐसा करने से न रोकें।
5. वित्तीय उपाय : आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों में बदलावों से ज्यादा टिकाऊपन की तरफ बढ़ने में मदद मिल सकती है। बहुत सारे गैर-सरकारी संगठनों की पुरजोर माँग है कि सरकारी रियातें रसायन सघन खेती जैसे विनाशकारी व्यवहारों की बजाय जैविक खेती जैसे टिकाऊ विकल्पों को मिलनी चाहिए। शहरी और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक मूल्य को इंगित करने वाले कर/टैक्स लागू किए जाएँ तो उपभोक्तावाद जैसी पर्यावरण-विनाशी परिघटनाओं को हतोत्साहित किया जा सकता है, आय असमानता पर अंकुश लगाया जा सकता है और पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है।
6. जागरूकता, शिक्षा, क्षमता : पर्यावरणीय एवं सामाजिक जागरूकता तथा सम्बन्धित समस्याओं से जूझने की क्षमताओं में पिछले दो-तीन दशकों के दौरान भारी इजाफा हुआ है। इसके बावजूद, निर्णयकारों और व्यवसाय जगत के शिखर पर बैठे लोगों के पास यह जागरूकता बहुत कम है। मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र की ओर संक्रमण के लिये विशाल अभियान चलाना होगा ताकि असंख्य संकटों और उनके कारणों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और उनके सार्थक समाधानों के प्रसार की क्षमता पैदा की जा सके।
 प्राकृतिक संसाधन अधिकारों पर गाँव में हो रही चर्चा, उड़ीसाभारत मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र की ओर बढ़ने के लिये सबसे अनुकूल स्थिति में हैं। इसके कई कारण हैं : भारत का हजारों साल लम्बा इतिहास व अनुकूलन की क्षमता (जिनमें प्राचीन लोकतांत्रिक आचार भी शामिल हैं जो सम्भवतः विख्यात ग्रीक रिपब्लिक से भी ज्यादा पुराने हैं), इसकी पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक विविधता, विविध संकटों के सामने इसका लचीलापन, नाना जीवन शैलियों व विश्व दृष्टिकोणों का बचे रहना जिनमें ऐसे प्रकृति-आश्रित समुदाय भी हैं जो आज भी धरती को बहुत कोमल हाथों से छूते हैं, बुद्ध, गांधी, टैगोर, अम्बेडकर और दूसरे प्रगतिशील चिन्तकों की शक्तिशाली विरासत, मार्क्स आदि अन्य चिन्तकों के क्रान्तिकारी विचारों का प्रयोग, लोकतंत्र व गैर-सरकारी संगठनों सक्रियता की प्रतिबद्धता और प्रतिरोध व पुनर्निर्माण के असंख्य जनान्दोलन इसकी थाती और विशेषता हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत अकेले इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उसे दूसरे देशों व समुदायों को भी समझाना, उनको बताना और उनसे सीखना होगा। ...और यह काम भी हम सदियों से बड़ी सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। अब हमें यही काम एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा कठिन माहौल में सम्पन्न करना है।
प्राकृतिक संसाधन अधिकारों पर गाँव में हो रही चर्चा, उड़ीसाभारत मूलभूत पर्यावरणीय लोकतंत्र की ओर बढ़ने के लिये सबसे अनुकूल स्थिति में हैं। इसके कई कारण हैं : भारत का हजारों साल लम्बा इतिहास व अनुकूलन की क्षमता (जिनमें प्राचीन लोकतांत्रिक आचार भी शामिल हैं जो सम्भवतः विख्यात ग्रीक रिपब्लिक से भी ज्यादा पुराने हैं), इसकी पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक विविधता, विविध संकटों के सामने इसका लचीलापन, नाना जीवन शैलियों व विश्व दृष्टिकोणों का बचे रहना जिनमें ऐसे प्रकृति-आश्रित समुदाय भी हैं जो आज भी धरती को बहुत कोमल हाथों से छूते हैं, बुद्ध, गांधी, टैगोर, अम्बेडकर और दूसरे प्रगतिशील चिन्तकों की शक्तिशाली विरासत, मार्क्स आदि अन्य चिन्तकों के क्रान्तिकारी विचारों का प्रयोग, लोकतंत्र व गैर-सरकारी संगठनों सक्रियता की प्रतिबद्धता और प्रतिरोध व पुनर्निर्माण के असंख्य जनान्दोलन इसकी थाती और विशेषता हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत अकेले इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उसे दूसरे देशों व समुदायों को भी समझाना, उनको बताना और उनसे सीखना होगा। ...और यह काम भी हम सदियों से बड़ी सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। अब हमें यही काम एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा कठिन माहौल में सम्पन्न करना है।
भारत में वैश्वीकरण प्रभाव और विकल्प (इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को पढ़ने के लिये कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें।) | |
1 | |
2 | |
3 | |




