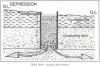Source
नया ज्ञानोदय 'बिन पानी सब सून' विशेषांक, मार्च 2004
 यह पानी भी विचित्र है—कभी हरहराती बाढ़, कभी रिमझिम-रिमझिम बारिश, कभी जलप्रलय और सृष्टि परिवर्तन, कभी धारासार वर्षा का रोमांस, कभी प्रेम की सरस बूँदों का स्पर्श, कभी नीर भरी दुख की बदली और कभी निर्झर-सा झरझर, कभी बादल का अमर राग- ‘झूम-झूम मृदु गरज-गरज घनघारे’ जो कृषकों को नयी आशा और जीवन देता है और कभी वही बादल मधुर गीत में ढल जाते हैं- ‘बादल छाए, ये मेरे अपने सपने, आँखों से निकले मँडलाए’, कभी वितस्ता की लहरें युद्धभूमि बन जाती हैं, कभी उमड़ती कुभा नदी का उफान युद्ध-संकट पैदा करता है। कालिदास का ‘मेघदूत’ हो या तानसेन का ‘मेघमल्हार’, ‘कामयनी’ की जल-प्रलय हो या ‘आषाढ़ का एक दिन’ का मेघ-गर्जन और वर्षा, वहाँ राग ही राग है, विश्व प्रेम पीयूष की वर्षा है और शताब्दियों के सपनों को पार करता है सागर, सागर की नन्ही, मंद लहर, फिर आकुल तरंग, फिर गम्भीर हिल्लोल। शिल्पी विशु की साधना और कला को, कोणार्क के खंडहर को वे साकार कर गयीं। लहरें ही सब कुछ कह गयीं-
यह पानी भी विचित्र है—कभी हरहराती बाढ़, कभी रिमझिम-रिमझिम बारिश, कभी जलप्रलय और सृष्टि परिवर्तन, कभी धारासार वर्षा का रोमांस, कभी प्रेम की सरस बूँदों का स्पर्श, कभी नीर भरी दुख की बदली और कभी निर्झर-सा झरझर, कभी बादल का अमर राग- ‘झूम-झूम मृदु गरज-गरज घनघारे’ जो कृषकों को नयी आशा और जीवन देता है और कभी वही बादल मधुर गीत में ढल जाते हैं- ‘बादल छाए, ये मेरे अपने सपने, आँखों से निकले मँडलाए’, कभी वितस्ता की लहरें युद्धभूमि बन जाती हैं, कभी उमड़ती कुभा नदी का उफान युद्ध-संकट पैदा करता है। कालिदास का ‘मेघदूत’ हो या तानसेन का ‘मेघमल्हार’, ‘कामयनी’ की जल-प्रलय हो या ‘आषाढ़ का एक दिन’ का मेघ-गर्जन और वर्षा, वहाँ राग ही राग है, विश्व प्रेम पीयूष की वर्षा है और शताब्दियों के सपनों को पार करता है सागर, सागर की नन्ही, मंद लहर, फिर आकुल तरंग, फिर गम्भीर हिल्लोल। शिल्पी विशु की साधना और कला को, कोणार्क के खंडहर को वे साकार कर गयीं। लहरें ही सब कुछ कह गयीं-दूर वह खंडहर सोता है,
पूरबी सागर के तट पर
सुनाती अगणित अथक लहर
मौन वह खंडहर सोता है।
पर जब उसी कोणार्क को युद्ध की विभीषिका से बचाना है तो अचानक प्रलयंकर और करुण संगीत के बीच वाचिका कहती है-
जूझते मेघों का गर्जन
भयंकर बिजली की तड़पन
रुधिर का उछला पारावार।
जब सब कुछ शांत हो जाता है तो स्तब्ध सरोवर की लहरें, क्षितिज पर चुपके से घिरते मेघ, उनके बीच दामिनी-मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। और पानी भी तो अथाह है, अनंत है। न जाने क्या-क्या कह जाता है! कोणार्क-जगदीशचंद्र माथुर
आषाढ़स्य प्रथम दिवसे! भीगा तन, भीगा मन, प्रेम का रस, बूँदों की पुलक! मल्लिका गीले वस्त्रों में काँपती-सिमटती अंदर आ रही है। क्षण भर ठिठकती है और फिर-
मल्लिकाः आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ?....ऐसी धारासार वर्षा! दूर-दूर तक की उपज्यकायें भीग गयीं।...और मैं भी तो! देखों न माँ, कैसी भीग गयी हूँ।
गयी थी कि दक्षिण से उड़कर आती वकुल-पंक्तियों को देखूँगी और देखो सब वस्त्र भिगो आयी हूँ।
तुम्हें पता था मैं भीग जाऊँगी। और मैं जानती थी कि तुम चिन्तित होगी। परन्तु माँ...मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं? भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती।
चारों ओर धुँआरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी। फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे-नीचे उतरती गयी। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूँदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत!
नील कमल की तरह कोमल और आद्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय! मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूँ और आँखें मूँद लूँ।....मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ! कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह! शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श! (गुनगुनाने लगती है)
कुवलयदल नीलैरुन्नतैस्तोयनम्रै....
गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ? यही रहने दूँ?
मृदुपवन विधूतैर्मन्दमन्दचलद्भि....
अपहृतमिव चेतस्तोयदैः.....सेनद्रचापै....
पथिकजनवधूनां तद्वियोगाकुलानाम्।
सौन्दर्य का अद्भुत अनुभव का ऐसा अस्पृश्य किन्तु मांसल साक्षात्कार। लेकिन देखो, इसी वर्षा ने बेचारे मातुल की क्या दुर्गति की है! पर इसी वर्षा और मेघ-गर्जन में ‘ऋतुसंहार’ के कवि कालिदास राजकवि का सम्मान प्राप्त करने पर मल्लिका के बहुत समझाने पर राजधानी जाते हैं तो-
...चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जयिनी की ओर उड़ जाएँगे....। मैं रो नहीं रही हूँ माँ! मेरी आँखों से जो बरस रहा है, यह दुःख नहीं है। यह सुख है माँ, सुख....।
वर्षों बाद उसी मेघ-गर्जन, बिजली की कौंध और वर्षा में भीगे क्षत-विक्षत कालिदास द्वार पर खड़े हैं।
कालिदास- जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्त्वाकांक्षा हो सकती है? वर्षों के बाद भीगा हूँ। अभी सूखना नहीं चाहता।
.....परन्तु मै। जानता हूँ। कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन ही संचय था। ‘कुमारसम्भव’ की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। ‘मेघदूत’ के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरहमर्दिता यक्षिणी तुम हो-
मल्लिका! मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीगता, भींगकर लिखता-वह सब जो मैं आज तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। परन्तु बरस नहीं पाता। क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती।
मल्लिका ने अपने हाथों से पन्ने सिये हैं कि कालिदास उन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करेंगे। कालिदास उन पृष्ठों पर मल्लिका के आँसू की बूँदे, स्वेदकण देखते हैं-ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है? इनपर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है....अनन्त सर्गों के एक महाकाव्य की। -आषाढ़ का एक दिन-मोहन राकेश
आह। रूपगर्विता सुंदरी को हंसों का कलरव और पंखों की फड़फड़ाहट कितनी अच्छी लग रही है? उतरती रात में लहरों में तैरते राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है।
सुंदरी- कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर है- ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किल्लोल ....कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमलताल के पास जाकर इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहें। ये एक बार चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर काँपती हुई लहरें जिधर ले जाएँगी, उधर को तैर जाएँगे। शायद उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी-तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि उस दिन....लेकिन अचानक पत्थर फेंकने का शब्द और उससे आहत हंसों का कम्पन?
-किसकी घृष्टता है यह? कमलताल में पत्थर कौन फेंक रहा है?
निश्चय ही यह आकस्मिक घटना नहीं है। जानबूझकर कामोत्सव की रात को ही किया गया प्रयत्न है।
 सचमुच क्या कुछ नहीं कह जाती लहरें (नन्द और सुंदरी की परिस्थितियाँ), राजहंस के जोड़े की किल्लोल (दोनों के आकर्षक सम्बम्ध का आनन्द), कमलताल (यह संसार) का पानी यहाँ प्रतीकों में? गौतम बुद्ध का निर्वाण सही है या सुंदरी का यौवन, रूप-गर्व यानी उसका पार्थिव रूप या गौतम बुद्ध की अपार्थिव दृष्टि?
सचमुच क्या कुछ नहीं कह जाती लहरें (नन्द और सुंदरी की परिस्थितियाँ), राजहंस के जोड़े की किल्लोल (दोनों के आकर्षक सम्बम्ध का आनन्द), कमलताल (यह संसार) का पानी यहाँ प्रतीकों में? गौतम बुद्ध का निर्वाण सही है या सुंदरी का यौवन, रूप-गर्व यानी उसका पार्थिव रूप या गौतम बुद्ध की अपार्थिव दृष्टि?और यह है शिप्रा नदी! शायद महाकवि कालिदास की रचना और कल्पनाओं की उड़ान से इसका गहरा रिश्ता है। रचनात्मक बेचैनी से, हलचल से शिप्रा तट की शान्ति, पानी और प्रकृति के रंग, कालिदास के भीतरी द्वंद्व और गहरे अँधेरे को विराम दे रहे हैं और वही शिप्रा, वही लहरें मन को नयी दिशा भी दिखा रही है-
कालिदास- पीछे शिप्रा नदी....अपनी ही गति पर मुग्ध प्रवाह....जल की अनवरत कलकल....सलोनी। निर्मल....मौलश्री के झुरमुट के पीछे डूबते-उतराते रंगों के इन्द्रधनुष....देखते-देखते मन विचलित हो गया....कि ऐसे पुनीत सम्मोहन को छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ मैं? ईष्या-द्वेष के उस छद्मलाख के घर में? दबावों और षडयंत्रों की उस मायानगरी में?.....मैं क्या करूँगा वहाँ?....यह सम्मान मुझे क्या देगा?....इस नाटक को जो देना है वह मुझे दे चुका है। -आठवाँ सर्ग सुरेन्द्र वर्मा
अरे! यह तो संशय की घनी रात में सिंधुतट पर अकेले टहलते राम हैं उदास, गरजते सागर को देखते हुए! बिलकुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे ‘राम की शक्ति पूजा’ में कवि निराला के राम। ‘स्थिर राघवेन्द्र को हिला रहा रह रह संशय।’ और कवि कह उठा-अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। यहाँ भी तो राम सिहराती सपाटे मारती हवा, वर्षा की रात में, एकांत में भाद्रपदी वृष्टि और विशाल रत्नाकर से सम्वाद करते हैं। जैसे दोनों उनके अकेलेपन के साथी बन गए-
ओ भाद्रपदी वृष्टि।
मुझे भी नारिकेलों सा
अभिषेकित हो जाने दो
आद्यन्त भीग उठने दो
उस आत्मा तक
जो खण्डित है
ओ भाद्रपदी वृष्टि।
आद्यन्त भीग उठने दो।
सम्भव है
तुम्हारे इन देवजलों से
यह संशयाग्नि शान्त हो सके
सम्भव है।
-संशय की एक रात-नरेश मेहता
और यह तो कुआँ है। कुएँ में पानी नहीं है पर वह है। उस अंधे कुएँ की सत्ता है। गाँव का परिवेश है, मिट्टी और बोली की गन्ध है, लोकसंगीत की लय है और है स्त्री की मार्मिक कथा, उसका दर्द, उसकी अन्तर्वेदना!-
कथाकार- हारने से पहले ही क्यों हार जाऊँ?
सूका ने सोचा फिर क्यों न भाग जाऊँ?
मगर इस बार वह किसी के संग न गयी भागकर वह कुएँ में कूद गयी।
मगर यहाँ भी किस्मत देखिए,
कुआँ अंधा था
कुआँ अंधा था
सब- कुआँ अंधा था
कुआँ अंधा था।
केहुना सुनी पुकार
हिरनी तब कुअँना गिरी
तुहिं राखो यहि बार
विरन गोसाई कुअँना।
-अंधा कुआँ-लक्ष्मीनारायण लाल
यह अंधा कुआँ! कितना अंधा, विवेकहीन, निर्दयी समाज! नियति बेचारी स्त्री की कि वह घूमफिरकर बार-बार फिर इसी कुएँ में गिरती है! कुएँ में पानी नहीं है पर वह है, उस अंधे कुएँ की सत्ता है।
पर यह कौन है? क्या नित्तिलाई? महाभारत के वनपर्व में एक छोटी-सी कथा है। अपने वनवास काल में देशाटन में पांडव इधर-उधर भटकते हैं। सन्त लोमष इन्हें यवक्री की कथा सुनाते हैं जिसके भीतर कई अर्थ छिपे हैं। इस छोटी-सी कथा पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। यवक्री और परावसु की उस कहानी से नाटककार सैंतीस वर्षों तक जूझता रहा और तब नित्तिलाई बोल पायी।
नित्तिलाई- मैं इतना ही तो कह रही हूँ कि इन्द्रदेवता ने यवक्री को दर्शन दिए। इन्द्र पानी का देवता है तो यवक्री इन्द्र देवता से यह क्यों नहीं कह देता कि थोड़ी-सी अच्छी-सी बरखा कर दो-अकाल पड़ा है? थोड़े मेघ बरसा दो। आप जाकर हमारा गाँव देखो, उसके चारों ओर का हाल देखो। पपड़ियाँ पड़ी हैं। दरक गयी है धरती। हर दिन सुबह-सवेरे मेरे बाबा के द्वारे लोग जमा हैं मुट्ठी-मुट्ठी भर दाने को, जो मेरा बाबा उन सूखी हथेलियों में डालता है। औरतों की हथेलियाँ जिनके सीने से भूखे बच्चे चिपके होते हैं- सूखे कंकाल-से बच्चे। कमान की तरह झुके हुए खोंखियाते बूढ़े-बूढ़ियाँ। एक भी जवान जैसे बचा ही नहीं हो! सब के सब नदारद हो गए जाने कहाँ? बाबा कहता है- इस धरती को चाहिए एक-दो झड़ी पानी मूसलाधार और तब धरती हरियाली। देवता से इतना भर माँगना भी बड़ी बात है क्या?
नित्तिलाई का स्पष्ट कहना है कि फिर ऐसी शक्तियों का फायदा ही क्या? क्या वह मेघ बरसा सकता है?
नाटक के अंत में बरखा होती है। भीड़ झूम उठती है।
भीड़- यह क्या है?....क्या गन्ध आती है तुम्हें उसकी? हाँ-हाँ, धरती के भीगने की गन्ध सौंधी-सौंधी महक माटी की। बरखा! पहली बूँद पड़ी हो जैसे। ओह, बरस रहा है यह तो! बरखा-पानी, कहीं न कहीं-आस-पास! हाँ, हवा में भर गयी है माटी की गन्ध। बरस राह है....बरस रहा है, बरखा, बरखा, पानी, पानी!
(हवा, बिजली, बादल की कड़क। लोगों का चीत्कार-बरखा। बरखा। राक्षस जैसे पिघल जाता है। उसकी हँसी का स्वर सुनायी देता है। ...मूसलधार बरखा सभी विभोर होकर नाच रहे हैं, माटी में लोट रहे हैं। माटी और पानी में बैठा है अरवसु नित्तिलाई के शव से लिपटा हुआ)अरवसु-देखो नित्तिलाई, बरखा! -अग्नि और बरखाः गिरीश करनाड
नेपथ्य से यह समूह मंत्रपाठ गूँज रहा है और सनतकुमार आम्रपल्लव से जल छिड़क रहे हैं।
यह जल कल्याणकारी है।
यह जल औषधियों की औषधि है।
यह जल राष्ट्र का संवर्द्धन करता है।
यह जल अमृतों का अमृत है।
-यमगाथाः दूधनाथ सिंह