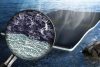हमारे देश में जल संसाधनों के प्रबन्धन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारतीय भागीरथों ने सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ भारत की जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य विविधताओं को ध्यान में रखकर बरसाती पानी, नदी-नालों, झरनों और जमीन के नीचे मिलने वाले, भूजल संसाधनों के विकास और प्रबन्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी।
हमारे देश में जल संसाधनों के प्रबन्धन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारतीय भागीरथों ने सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ भारत की जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य विविधताओं को ध्यान में रखकर बरसाती पानी, नदी-नालों, झरनों और जमीन के नीचे मिलने वाले, भूजल संसाधनों के विकास और प्रबन्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। जल संसाधनों से जुड़ा यह प्रबन्धन वर्ष के अधिकांश दिनों तक बर्फ से ढके लद्दाख से लेकर दक्षिण के पठार तथा थार के शुष्क मरुस्थल से लेकर अति वर्षा वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशिष्ट और स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त था। इन सभी स्थानों पर वहाँ की जलवायु और पानी अथवा बर्फ की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जल संचय, उसके निस्तार और सिंचाई में उपयोग के तौर-तरीके खोजे गए थे। तथा समय की कसौटी पर खरी विधियाँ विकसित की गई थीं।
इन उपलब्धियों के पुष्ट प्रमाण देश के कोने-कोने में उपलब्ध हैं। वस्तुतः ये प्रमाण भारतीय भागीरथों के उन्नत ज्ञान, दूरदृष्टि और परिस्थितियों की बेहतरीन जानकारी को दर्शाते हैं तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक हैं।
जल प्रबन्धन का पहला प्रमाण सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान मिला। धौरावीरा में अनेक जलाशयों के प्रमाण भी मिले हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार कुएँ बनाने की कला का विकास भी हड़प्पा काल में हुआ था। इस क्षेत्र में हुई खुदाई तथा सर्वेक्षणों से विदित हुआ है कि वहाँ हर तीसरे मकान में कुआँ था।
ईसा के जन्म से लगभग 300 वर्ष पूर्व कच्छ और बलूचिस्तान के लोग बाँध बनाने की कला से परिचित थे। उन्होंने कंकड़ों और पत्थरों की सहायता से बहुत ही मजबूत बाँध बनाए थे और उनमें वर्षाजल को संरक्षित किया था। बाँधों में संरक्षित यह पानी पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काम में लाया जाता था और लोग बाँध में एकत्रित पानी के प्रबन्धन में दक्ष थे।
चन्द्रगुप्त मौर्य (ईसा से 321-297 वर्ष पूर्व) के कार्यकाल में भारतीय किसान सिंचाई के साधनों, यथा - तालाब, बाँध इत्यादि से न केवल परिचित था वरन वर्षा के लक्षण, मिट्टी के प्रकार और जल प्रबन्धन के तरीकों को भी अच्छी तरह से जानता था।
जल विज्ञान और जल प्रबन्धन के कार्य से जुड़े ज्ञान में पारंगत होने के कारण, समाज, संरचनाओं को बनाने, चलाने और अनुरक्षण के कार्य को अंजाम भी देता था। उस काल के राजा का कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करना था।
 उस काल के लोग बाढ़ नियंत्रण के कार्य से भी अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने ईसा के जन्म से एक शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के पास गंगा की बाढ़ से बचने के लिये नहरों और तालाबों की एक दूसरे से जुड़ी संरचनाएँ बनाई थीं। इन संरचनाओं के कारण गंगा की बाढ़ का अतिरिक्त पानी कुछ समय के लिये इन नहरों और तालाबों में एकत्रित हो जाता था। इस प्रणाली के अवशेष श्रृंगवेरपुरा में प्राप्त हुए हैं।
उस काल के लोग बाढ़ नियंत्रण के कार्य से भी अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने ईसा के जन्म से एक शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के पास गंगा की बाढ़ से बचने के लिये नहरों और तालाबों की एक दूसरे से जुड़ी संरचनाएँ बनाई थीं। इन संरचनाओं के कारण गंगा की बाढ़ का अतिरिक्त पानी कुछ समय के लिये इन नहरों और तालाबों में एकत्रित हो जाता था। इस प्रणाली के अवशेष श्रृंगवेरपुरा में प्राप्त हुए हैं।पारम्परिक जल संरक्षण प्रणालियों की प्रासंगिकता
जल संचय और प्रबन्धन का चलन हमारे यहाँ सदियों पुराना है। राजस्थान में खड़ीन, कुंड और नाडी, महाराष्ट्र में बन्धारा और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बन्धी, बिहार में आहर और पइन, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में एरी, केरल में सुरंगम, जम्मू क्षेत्र के कांडी इलाके के पोखर, कर्नाटक में कट्टा पानी को सहेजने और एक से दूसरी जगह प्रवाहित करने के कुछ अति प्राचीन साधन थे, जो आज भी प्रचलन में हैं।
पारम्परिक व्यवस्थाएँ उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और संस्कृति की विशिष्ट देन होती है, जिनमें उनका विकास होता है। वे न केवल काल की कसौटी पर खरी उतरी हैं, बल्कि उन्होंने स्थानीय जरूरतों को भी पर्यावरण में तालमेल रखते हुए पूरा किया है। आधुनिक व्यवस्थाएँ जहाँ पर्यावरण का दोहन करती हैं, उनकी विपरीत यह प्राचीन व्यवस्थाएँ पारिस्थितिकीय संरक्षण पर जोर देती है। पारम्परिक व्यवस्थाओं को अनन्त काल से साझा मानवीय अनुभवों से लाभ पहुँचता रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।
भारत में वर्षा बहुत ही मौसमी होती है। देश में कुल वार्षिक वर्षा 1,170 मिमी होती है, वह भी केवल तीन महीनों में। देश के 80 प्रतिशत हिस्से में इस वर्षा का 80 फीसदी भाग इन्हीं तीन महीनों में गिरता है। बरसात के मौसम में पूरी वर्षा 200 घंटे होती है और इसका आधा हिस्सा 20-30 घंटों में होता है। परिणामतः वर्षा का बहुत ज्यादा पानी बेकार बह जाता है।
भारी वर्षा के दौरान नदियों के बाँध भी वहाँ से बह जाने वाले पानी का मात्र 20 फीसदी या उससे भी कम जमा कर पाते हैं। बाकी 80 फीसदी पानी भी बिना उपयेाग के बह जाने दिया जाता है, ताकि बाँध को क्षति न पहुँचे।
जल संचयन का सिद्धान्त यह है कि वर्षा के पानी को स्थानीय जरूरतों और भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से संचित किया जाय। इस क्रम में भूजल का भण्डार भी भरा जाता है। जल संचयन की पारम्परिक प्रणालियों से लोगों की घरेलू और सिंचाई सम्बन्धी जरूरतें पूरी होती रही हैं।
उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि ई.पू चौथी शताब्दी से ही देश के कई क्षेत्रों में छोटे-छोटे समुदाय जल संचय और वितरण की कारगर व्यवस्था करते रहे। नंद के शासन में (363-321 ई.पू.) शासकों ने नहरें और समुदाय पर निर्भर सिंचाई प्रणालियाँ बनाईं। मध्य भारत के गौड़ शासकों ने सिंचाई और जल आपूर्ति की न केवल बेहतर प्रणालियाँ बनाईं, बल्कि उनके रख-रखाव के लिये आवश्यक सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी विकसित की थीं।
 सम्भव है कि प्राचीन समय की इन जल संचयन प्रणालियों से पानी का समान बँटवारा न होता हो। लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इन पारम्परिक प्रणालियों के सामुदायिक प्रबन्धन के कारण हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होती थीं।
सम्भव है कि प्राचीन समय की इन जल संचयन प्रणालियों से पानी का समान बँटवारा न होता हो। लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इन पारम्परिक प्रणालियों के सामुदायिक प्रबन्धन के कारण हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होती थीं।सभी प्रारम्परिक प्रणालियाँ छोटी नहीं थी। शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिये बड़ी प्रणालियाँ भी बनाई जाती थीं। लेकिन छोटी प्रणालियों के साथ इनका तालमेल होता था, जैसा कि चोल काल (930-1200 ई.) और मध्यकालीन विजयनगर में दिखता है। प्राचीनता का गुणगान किये बिना कहा जा सकता है कि पानी आपूर्ति और पूँजी पर लाभ के लिहाज से पारम्परिक प्रणालियाँ तब भी ज्यादा कारगर थी और आज भी है।
यह प्रणालियाँ इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि सूखे या अकाल के लम्बे दौर में भी उन्होंने समुदायों को जीवनदान दिया है। लेकिन कभी-कभी जब वर्षों तक वर्षा नहीं होती थी तो छोटी प्रणालियाँ नाकाम हो जाती थीं। इससे बड़ी प्रणालियों की जरूरत बन जाती। लेकिन छोटी और बड़ी प्रणालियों के बीच सन्तुलन सावधानी के साथ बनाए रखा जाता था। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रणालियों के नियोजन और क्रियान्वयन में ग्रामीण और शहरी दोनों समुदाय भाग नहीं लेते। इस तरह, अतीत हमें भविष्य के लिये सबक देता है।
आज, लोग आधुनिक प्रणाली चाहते हैं, क्योंकि जब घर में नल खोलते ही पानी आ सकता है तो कुएँ या तालाब से पानी लाने के लिये पैदल चलना कौन चाहेगा। इसी तरह सिंचाई के लिये पम्पसेट का बटन दबाते ही या बाँध का दरवाजा खोलते ही पानी पाना हर कोई चाहेगा। लेकिन जब नल सूखता है और बाँध में मिट्टी भरने लगती है और आधुनिक प्रणालियाँ नाकाम होने लगती हैं तब लोगों को पारम्परिक प्रणालियों की सुध आती है।
देश का बड़ा हिस्सा ऐसा भी जहाँ आधुनिक प्रणालियाँ भारी लागत की वजह से पहुँच ही नहीं सकती। इस हिस्से में लोग पीने के पानी और सिंचाई के लिये पारम्परिक प्रणालियों पर ही निर्भर है। आधुनिक प्रणालियों के साथ दूसरी समस्या यह है कि इन्होंने सरकार पर ग्रामीण समुदायों की निर्भरता बढ़ा दी है।
पारम्परिक प्रणालियों का अर्थ पुराना, जर्जर ढाँचा नहीं है। ये प्रणालियाँ सरकार द्वारा नियंत्रित प्रणालियों से भिन्न हैं। आधुनिक प्रणालियाँ ऊँची लागत वाली तो होती ही हैं, पर्यावरण के सन्दर्भ में भी बड़ी कीमत वसूलती हैं। इनसे मिले पानी का उपयोग आमतौर पर मौसम के अनुकूल खेती के बुनियादी मानदण्डों के विपरीत होता है। नलकूपों से भारी मात्रा में भूजल निकाला जा रहा है।
कई सरकारी एजेंसियाँ यह नहीं समझतीं की वे जिन स्रोतों से पानी खींच रही है, इन स्रोतों से निरन्तर पानी मिलता रहेगा। समुदाय पर आधारित पारम्परिक प्रणालियाँ सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता को भी बल देती है। इनमें फैसले करने का अधिकार प्रायः व्यक्तियों, समूह या स्थानीय समुदायों को दिया जाता था, जो साथ मिलकर काम कर रहे होते थे। इससे आर्थिक स्वाधीनता बढ़ती थी और नीचे के स्तर पर स्थानीय संसाधनों का पूरा-पूरा इस्तेमाल होता था।
पारम्परिक प्रणालियों में सस्ती, आसान तकनीक का प्रयोग होता था जिससे स्थानीय लोग भी आसानी से कारगर बनाए रख सकते थे। आधुनिक प्रणालियों ने समुदायों को तोड़ दिया और बाजार के सिद्धान्तों पर चलने वाली आधुनिक प्रणालियाँ वितरण के मोर्चे पर कच्ची साबित हुई है।
 पानी आर्थिक विकास का मेरूदण्ड है। जल संसाधनों का यदि समतामूलक, समुदाय आधारित और व्यावहारिक ढंग से विकास करना है तो पारम्परिक प्रणालियों को सशक्त बनाना होगा और उनका विकास करना होगा।
पानी आर्थिक विकास का मेरूदण्ड है। जल संसाधनों का यदि समतामूलक, समुदाय आधारित और व्यावहारिक ढंग से विकास करना है तो पारम्परिक प्रणालियों को सशक्त बनाना होगा और उनका विकास करना होगा।भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित जल संरक्षण की प्रणालियाँ
भारत को जलवायुवीय एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से पाँच भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें वर्षा के वितरण एवं मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की जल संरक्षण प्रणालियाँ विकसित कर रखी हैं। इनके बारे में जानकारी निम्नवत है-
1. हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जल संरक्षण व्यवस्था
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें विभिन्न भौगोलिक दशाओं एवं जल प्राप्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की जल संचयन की प्रणालियाँ प्रचलित हैं। जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में कुहल प्रणाली पाई जाती है। यह प्रणाली नहरी तंत्र की तरह ही विकसित की गई है। यह पहाड़ी धाराएँ 15 किलोमीटर तक लम्बी होती है। कुहल से जुड़ी कच्ची नालियों को मोघा कहते है।
कुहल नामक प्रणाली द्वारा हिमनदी का पिघला पानी बहकर तालाबों में संचित होता है यह हिमपात के समय तीव्र गति से बहते हैं तथा ठंडे समय में इसमें पानी की कम मात्रा आती है। इसके पानी के उपयोग हेतु बँटवारा निश्चित कर दिया जाता है। प्रति कुहल के निर्माण पर 3000 से 5000 रु. तक की लागत आती है। मण्डी में कुहलों का निर्माण प्राचीन समय में माल गुजारों एवं ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था।
लद्दाख क्षेत्र में लोगों द्वारा ऐसा ही मार्ग विकसित किया जाता है, जिसे जिंग कहते है, जिंग के पानी का बँटवारा चुरपुन नामक अधिकारी द्वारा किया जाता है। लाहोल एवं स्फीती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के रास्ते विकसित किये गए थे जिनसे होकर बर्फ पिघलकर गाँवों में पानी के रूप में पहुँचती है। यह काफी लम्बे एवं असम क्षेत्रों में विकसित होते है। इनका मुख्य भाग हिमनदों का मुहाना होता है जहाँ पानी संरक्षित होता है।
इस रास्ते में पानी के रिसाव को रोकने हेतु पार्श्वों एवं तलीय भागों में पत्थर बिछाए जाते थे। इस प्रणाली को कूल कहते है। कूल प्रणाली पारस्परिक सहयोग एवं साझेदारी पर आश्रित रहता है। वर्तमान समय में इनका सरकारीकरण होने से इनके प्राचीन अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है।
कई जगह हिमाचल सरकार इनकी मरम्मत भी करवा रही है, किन्तु इनका स्वरूप आधुनिक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन तालाबों एवं अन्य छोटे कुओं को नौला या होजी कहते हैं, जो इस क्षेत्र की परम्परागत जल संचय की उपयुक्त प्रणाली है। इनके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। होजी के निर्माण में धार्मिक तत्वों का भी योगदान माना गया है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही प्रणाली को ‘हारा प्रणाली’ कहते हैं।
पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग में झोरों (झरनों से) सिंचाई होती है। इनसे बाँस के पाइपों द्वारा पानी को सीढ़ीदार खेतों तक पहुँचाया जाता है। झोरा विधि को लेप्या, भोटिया एवं गुरूंग लोगों ने जीवित रख रखा है। सिक्किम मे पेयजल के लिये झरनों एवं खोलों (तालाबों) का जल प्रयोग में लिया जाता है। इन तालाबों में बाँस के पाइपों से जल पहुँचाया जाता है। पेयजल हेतु घरों के आहाते में जल कुंडियाँ बनाते हैं जिन्हें खूप कहते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में बाँस की नालियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यहाँ की नालियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यहाँ सुबनसिरी जिले में केले नदी पर अपतानी आदिवासियों द्वारा परम्परागत प्रणाली से सुबनसिरी जिले में केले नदी पर अपतानी आदिवासियों द्वारा परम्परागत प्रणाली से बाँध बनाए गए है। यहाँ झरनों के पानी का संचय किया जाता है, जिनमें मछली पालन भी किया जाता है।
 अपतानी लोग पानी संचय करने के मार्ग गाँव के पास से बनाते हैं ताकि गाँव में से मनुष्यों एवं पशुओं का मल-मूत्र इस सिंचाई जल में मिलने से यह उर्वरक बन गए। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैण्ड की ‘जाबो’ प्रणाली प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय भाषा में रूजा प्रणाली भी कहते हैं। यह कृषिवानिकी और पशुपालन की मिश्रित प्रणाली है, जो जल संरक्षण की प्रभावकारी पद्धति है। क्रिकुमा गाँव के ये लोग जल संरक्षण में बहुत माहिर होते हैं। वे पानी को सड़क के किनारे संग्रहित करके तालाब तक ले जाते हैं।
अपतानी लोग पानी संचय करने के मार्ग गाँव के पास से बनाते हैं ताकि गाँव में से मनुष्यों एवं पशुओं का मल-मूत्र इस सिंचाई जल में मिलने से यह उर्वरक बन गए। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैण्ड की ‘जाबो’ प्रणाली प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय भाषा में रूजा प्रणाली भी कहते हैं। यह कृषिवानिकी और पशुपालन की मिश्रित प्रणाली है, जो जल संरक्षण की प्रभावकारी पद्धति है। क्रिकुमा गाँव के ये लोग जल संरक्षण में बहुत माहिर होते हैं। वे पानी को सड़क के किनारे संग्रहित करके तालाब तक ले जाते हैं। इन जल संग्रह स्थलों की समयानुसार मरम्मत भी करवाई जाती है। मेघालय में झरनों के पानी को बाँस की नालियों के द्वारा सिंचाई के लिये ले जाते हैं। यह प्रणाली वर्तमान बूँद-बूँद सिंचाई प्रणाली के समान होती है। इन नालियों में प्रति मिनट 18 से 20 लीटर पानी निकलता है। इस प्रकार यहाँ बाँस से ड्रिप सिंचाई की जाती है। यह प्रणाली गारों, वार एवं खासी क्षेत्रों में प्रचलित है।
जलमार्ग बनाने के लिये विभिन्न व्यास के बाँसों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली को बनाने से पहले बाँस को छिलकर पतला किया जाता है और इसके बीच में बनी गाँठों को हटा दिया जाता है। उसके बाद स्थानीय कुल्हाड़े-दाब से उन्हें चिकना बनाया जाता है। इसके बाद मुख्य मार्ग से पानी को विभिन्न जगहों पर ले जाने और वितरित करने के लिये छोटी-छोटी नालियों का प्रयोग किया जाता है।
नाली में पानी के प्रवेश करने से लेकर उसके पौधों के पास पहुँचने तक कुल 4 या 5 चरण होते हैं। पौधों की जड़ों के पास पानी बूँद-बूँद पहुँचे इसके लिये हर स्तर पर बुद्धिमता के साथ पानी का प्रभाव मोड़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि एक हेक्टेयर भूमि में ऐसी प्रणाली बनाने के लिये दो मजदूरों को 15 दिनों तक काम करना पड़ता है। वैसे यह श्रम पानी के स्रोत की दूरी और सिंचित होने वाले पौधों की संख्या पर निर्भर करता है। एक बार यह प्रणाली लग जाये तो उसके ज्यादातर सामान लम्बे समय तक टिकते हैं।
2. गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान
भारत में गंगा का मैदानी क्षेत्र छोटी-छोटी नदियों का वृहद क्षेत्र है। इस मैदान की सभ्यता में नदियों का अधिक योगदान है। पंजाब में परम्परागत प्रणालियों में नहरें, कुएँ एवं झालरें प्रमुख हैं। झालरें कम गहराई वाले चौड़े कुएँ होते हैं। यहाँ तालाबों में नहरें, कुएँ एवं झालरें प्रमुख हैं। झालरें कम गहराई वाले चौड़े कुएँ होते है। यहाँ तालाबों से मोटर से पानी निकालकर उपयोग में लेते हैं।
हरियाणा में कुओं, नहरों के अतिरिक्त आबी में जल का संचय किया जाता है। आबी एक प्रकार का तालाब होता है, जिसमें वर्षाजल को संग्रहित किया जाता है। दिल्ली का सूरजकुण्ड भी परम्परागत जल संचय का उदाहरण है, जिसमें अरावली के उत्तरी भाग से पानी आता है। महरौली के पास हौज-ए-शम्सी जलाशय (शम्सी झील) में भी जल संचय किया जाता है। इनके अतिरिक्त दिल्ली में यमुना नदी प्रमुख जलस्रोत है, जिसको अब प्रदूषित कर दिया गया है।
यमुना दिल्ली में 48 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, जिसका प्राचीन स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में जोहड़ों में पानी को संग्रहित किया जाता है यह जोहड़ महाभारत काल से ही बनते रहे हैं। जिनकी सफाई समय-समय पर की जाती थी लेकिन वर्तमान समय में यह जोहड़ काफी प्रदूषित हो गए हैं। इनमें काचला का जोहड़ प्रमुख है।
बिहार की आहर-पइन व्यवस्था भी परम्परागत जल संचय का उत्तम उदाहरण है। आहर तीन ओर से जल से घिरी हुई आयताकार आकार में होती है जिनसे पइन द्वारा जल खेतों तक पहुँचाया जाता है। आहर-पइन व्यवस्था का उपयोग सर्वप्रथम जातक युग में आरम्भ हुआ था। इसका उपयोग लोग मिल जुलकर किया करते थे लेकिन निरन्तर बाढ़ों के कारण इनका प्राचीन स्वरूप परिवर्तित हो गया है।
ब्रह्मपुत्र मैदान में जाम्पोई विधि द्वारा जल का संचय किया जाता है। यह विधि पश्चिमी बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में प्रचलित है। जाम्पोई विधि में जल संग्रह के लिये छोटी-छोटी नालियाँ बनाई जाती है। जिन्हें दूंग कहते थे। वर्तमान समय में वनों के कटने के कारण इनका आकार बदल रहा है, क्योंकि बाढ़ भी अधिक आने लगी है। इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में छोट-छोटी नदियों से जल संरक्षण किया जाता था जिनमें काणा, कुन्ती, दामोदर प्रमुख है जिनसे ढेंकली से जल निकालते थे।
आसाम में अहोम राजाओं द्वारा जल संचयन का अच्छा प्रयास किया गया था उनके समय में पोखरों का निर्माण किया गया था। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा पोखरों का निर्माण किया गया जिन्हें डोग कहते हैं। इन तालाबों से लाहोमियों द्वारा चंवर-चाचर विधि द्वारा जल लिया जाता है।
3. पठारी भाग
पठारी भागों में मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली व कर्नाटक की केरे प्रणाली प्रमुख है। जबलपुर में ऊँचे बाँधों द्वारा वर्षा के पानी को बाँधा जाता है, जो फसल बोने तक खेतों में रहता है। इसको रोकने के लिये खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है जिसे बंधारे कहते हैं। जिसकी समय-समय पर मरम्मत की जाती है। मध्य प्रदेश में मुगलकालीन जल प्रबन्धन की व्यवस्था मिलती है। बुरहानपुर में भण्डारों में जल संग्रह किया जाता था।
 भण्डारा वर्तमान ऐनीकट के सदृश्य होते थे। इन भण्डारों से जल नालियों द्वारा भूमि के अन्दर होता हुआ शहर तक पहुँचता था। इन भूमिगत मार्गों को जलकरंज कहते थे। इन जलकरंजों के मध्य प्रति 20 मीटर पर हवा आने-जाने के लिये वायु कूपक रखे जाते थे। यह सम्पूर्ण प्रणाली गुरुत्वार्षण प्रणाली पर आधारित थी। इस व्यवस्था को भी वर्तमान प्रदूषण का शिकार होना पड़ा है। झाबुआ में पहाड़ियों के अन्दर पानी को विशिष्ट प्रकार की नालियों की ओर मोड़ देते हैं। जिन्हें पाट कहते थे।
भण्डारा वर्तमान ऐनीकट के सदृश्य होते थे। इन भण्डारों से जल नालियों द्वारा भूमि के अन्दर होता हुआ शहर तक पहुँचता था। इन भूमिगत मार्गों को जलकरंज कहते थे। इन जलकरंजों के मध्य प्रति 20 मीटर पर हवा आने-जाने के लिये वायु कूपक रखे जाते थे। यह सम्पूर्ण प्रणाली गुरुत्वार्षण प्रणाली पर आधारित थी। इस व्यवस्था को भी वर्तमान प्रदूषण का शिकार होना पड़ा है। झाबुआ में पहाड़ियों के अन्दर पानी को विशिष्ट प्रकार की नालियों की ओर मोड़ देते हैं। जिन्हें पाट कहते थे।महाराष्ट्र में फड़ प्रणाली परम्परागत तरीके से जल संचय की उपयुक्त प्रणाली है। इसका इतिहास 300 से 400 वर्ष पुराना है, जब इनका विकास सर्वप्रथम नासिक एवं धुले जिलों में हुआ। बन्धारा एक से अधिक गाँवों को जल आपूर्ति करता था। इनका रख-रखाव जिसकी भूमि होती थी वहीं किया करता था।
4. तटीय मैदान एवं द्वीप समूह
पश्चिमी तटीय भागों में गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में भूजल काफी ऊँचा है तथा यहाँ पर जल संचयन हेतु बावड़ियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें वाव कहते हैं। इन वावों से चड़स द्वारा पानी खींच कर उपयोग में लेते हैं। अहमदाबाद में पन्द्रहवीं सदी में अनेक ताबाल बने थे, जिनमें से अधिकांश को सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कराया था। यहाँ की मानसर झील प्रसिद्ध है, जिसमें वर्ष भर जल रहता है। इसका क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है। इसमें पानी कुंड से आता है। खेड़ा, बड़ोदरा व कारावन में भी काफी मात्रा में तालाब विद्यमान हैं।
महाराष्ट्र के विस्तृत मैदान में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों-वैतरणी, उल्हास, तसां, सावित्री और वशिष्टी प्रवाहित होती है। इनके अतिरिक्त तालाब एवं झीलों में भी वर्षाजल को एकत्रित करते हैं। यहाँ खेतों के मेड़ बनाकर पारम्परिक ढंग से वर्षों के जल को रोकते हैं। कोंकण में अनेक जलाशय हैं, जिनका निर्माण हिन्दू शासकों एवं परोपकारी लोगों ने करवाया था, इनमें बोराला, पाथरड़ी, नागेश्वर व काशर जलाशय प्रसिद्ध है।
महाराष्ट्र के ठाणे एवं कुलाबा में समुद्री ज्वार से आये पानी को खेतों में सिंचाई हेतु बाँधों में संरक्षित किया जाता था। इस प्रणाली को ‘शिलोत्री’ कहते हैं, जिसका प्रारम्भ मराठा शासकों द्वारा सर्वप्रथम किया गया। केरल का 60 प्रतिशत से अधिक धरातल पथरीला है, जिससे जलाशय निर्माण में कठिनाई आती है। इसी कारण केरल पानी में रहकर भी प्यासा है। यहाँ मानसून काल में प्राप्त वर्षाजल को संग्रहित करने की व्यवस्थाओं का अभाव है।
पूर्वी तटीय मैदान में पालर से जुड़ी प्रणालियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पालर नदी कर्नाटक में नदी की पहाड़ियों से निकलकर 350 किलोमीटर बहकर तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। चितूर जिले में इसका उपयोग भूजल स्तर बढ़ाने में किया गया है। तमिलनाडु में इसके जल को पीने के काम में लेते हैं।
पालर नदी के पास कासम प्रणाली कायम है। कासम प्रणाली एक लम्बा तालाब होता है, जो नदी तल से नीचे बनाया जाता है। जिसमें नदी का पानी रिसकर संग्रहित होता रहता है। इस नदी बेसिन में लोगों ने कई प्रकार की जलसंग्रह की व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। जिनमें रेवु, दोन, ओडू, गोकूटां, कुटां एवं चेरूवु मुख्य है। रेवु प्रणाली झरनों से पानी संग्रह की प्रणाली थी जो पत्थर, मिट्टी और घास से बनाई जाती थी।
दोन छोटे पोखर थे, जो चट्टानों के प्राकृतिक गड्ढों से बनते थे। इनका पार्श्व पथरीला होने के कारण पानी नहीं रिसता था व लम्बे समय तक रहता था। ओडू प्रणाली में नदी या सोते के ऊपर एनीकट के रूप में दीवार बनाई जाती थी, जिसका अधिकांश पानी सिंचाई के काम आता था। मवेशियों के उपयोग हेतु बनाए गए तालाबों को गोकुटां कहते थे जो सामान्यतया जंगल में चारागाहों के पास बनाए जाते थे, जबकि कूंटा वर्षाजल को तालाब में संचित करने की प्रणाली थी जिसका उपयोग घरेलू कार्यों एवं मवेशियों हेतु किया जाता था।
 कूंटा में जलसंग्रह से भूजल में बढ़ोतरी के साथ ही बाढ़ पर भी नियंत्रण लगता था। पालर बेसिन में सिंचाई हेतु बनाए गए तालाबों को चेरूवु कहते थे, जो सोतो (वागु) के ऊपर एनीकट बनाकर पानी रोककर बनाए जाते थे। इन पारम्परिक जल संग्रह प्रणालियों की वर्तमान में उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण हालत खराब हैं।
कूंटा में जलसंग्रह से भूजल में बढ़ोतरी के साथ ही बाढ़ पर भी नियंत्रण लगता था। पालर बेसिन में सिंचाई हेतु बनाए गए तालाबों को चेरूवु कहते थे, जो सोतो (वागु) के ऊपर एनीकट बनाकर पानी रोककर बनाए जाते थे। इन पारम्परिक जल संग्रह प्रणालियों की वर्तमान में उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण हालत खराब हैं।तमिलनाडु की पारम्परिक जल संग्रह तकनीक तालाबों में देखने को मिलती है। तमिलनाडु का 35 प्रतिशत भाग तालाबों से सिंचित है। इन्हें एरी कहते हैं। एरी के निर्माण द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण होने से भूक्षरण रुकता है तथा व्यर्थ बहने वाला वर्षाजल संग्रहित किया गया जिससे भूजल भण्डार ऊपर उठे हैं। एरी के रख-रखाव की व्यवस्था 16वीं शताब्दी में विद्यमान थी।
चेंगलपट्ट जिले के मदुरन्तकम एरी के ऐतिहासिक आँकड़ों से विदित हुआ है कि प्रत्येक गाँव के कुल उत्पादन का 20वाँ हिस्सा एरी रख-रखाव एवं सिंचाई पर खर्च किया जाता था। अंग्रेजी शासन आते ही इन पारम्परिक जलस्रोतों का पतन आरम्भ हो गया । 80 के दशक से एरी के आधुनिकीकरण का अभियान चल रहा है। तथा वर्तमान रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र को सौंपी गई है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ परम्परागत जल संग्रह पद्धतियों को संरक्षित करने में दक्ष हैं यहाँ सोपेन और जारवा आदिवासी बाँस को चीरकर उसका उपयेाग करके जलसंग्रह करते है। बाँस को काटकर ढाल के अनुसार नीचले स्थानों पर स्थित किया जाता है जिनके द्वारा बिखरता बरसाती पानी छिछले गड्ढों में संग्रहित हो जाता है, जिन्हें ‘जैकवेल’ कहते है।
फटे बाँसों को पेड़ों के नीचे भी बिछाया जाता है जिनसे पत्तियों का पानी संग्रहित किया जाता है। जैकवेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिनमें एक गड्ढा भरकर दूसरे में जल जाता रहता है तथा अन्त में बड़े जैकवेल में जमा हो जाता है। यहाँ बाँस तकनीक के अतिरिक्त नारियल वृक्षों के नीचे बर्तन या घड़ा रखकर भी जलसंग्रह किया जाता है। ओंगी आदिवासियों द्वारा छतों से गिरने वाले पानी को बर्तनों में भरकर संग्रह किया जाता है।
भारत के प्रवाल स्वर्ग लक्षद्वीप में पेयजल के लिये कुओं, बावड़ियों एवं तालाबों का विकास किया गया है। कबरती में लगभग 800 कुएँ है। घरेलू उपयोग हेतु मुख्यतया तालाबों एवं बावड़ियों का प्रयोग करते हैं। इन व्यवस्थाओं के बाद भी लक्षद्वीप में जल का संकट व्याप्त है। तथा इस संकट से निजात वर्षा के पानी को संचित करके ही पाया जा सकता है।
उपर्युक्त पारम्परिक जलसंग्रह की प्रणालियाँ काल की कसौटी पर खरी उतरी हैं। यह प्रणालियाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अपने प्रभावकारी स्वरूप में उभरी हैं। इनका विकास स्थानीय पर्यावरण के अनुसार हुआ है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित यह प्रणालियाँ अपने विशिष्ट स्वरूप में उभरी हैं, जिनमें राजस्थान की पारम्परिक जल संचय विधियाँ अपनी अलग विशेषताएँ रखती हैं। जिनके विकास में ऐतिहासिक तत्वों के साथ विविध भौगोलिक कारकों का प्रभाव प्रमुख है।
TAGS |
various traditional ways water harvesting (information in Hindi), traditional water storage (information in Hindi), catching rainwater traditional methods (information in Hindi), traditional water harvesting structures (information in Hindi), traditional water harvesting techniques (information in Hindi), rainwater harvesting tanks (information in Hindi), water harvesting method traditional and modern (information in Hindi), traditional water harvesting techniques (information in Hindi), traditional water harvesting structures (information in Hindi), old methods of rainwater harvesting (information in Hindi), traditional water storage (information in Hindi), traditional ways of water harvesting wikipedia (information in Hindi), ancient methods of rainwater harvesting (information in Hindi), modern methods of water harvesting (information in Hindi), Traditional Water Harvesting Systems of India (information in Hindi), catching rainwater traditional methods (information in Hindi), water harvesting structures ppt (information in Hindi), old water harvesting structures planning design and construction (information in Hindi), old water harvesting structures watershed (information in Hindi). |