 5 सितम्बर 1984 को सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में हेमपुर गाँव के पास कोसी नदी का तटबंध टूटा था और कोसी ने 196 गाँवों को अपनी आगोश में ले लिया था। करीब 5 लाख लोग तटबंध के बचे हुए हिस्से पर शरण लिये हुए थे। दूर तक पानी और सिर्फ पानी ही दिख रहा था। पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ था।
5 सितम्बर 1984 को सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में हेमपुर गाँव के पास कोसी नदी का तटबंध टूटा था और कोसी ने 196 गाँवों को अपनी आगोश में ले लिया था। करीब 5 लाख लोग तटबंध के बचे हुए हिस्से पर शरण लिये हुए थे। दूर तक पानी और सिर्फ पानी ही दिख रहा था। पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ था।
उसी वक्त एक 38 वर्षीय इंजीनियर के पास संदेश आता है कि सहरसा में कुछ समस्याएँ हैं और उसे वहाँ जाकर काम करना है। संदेश देनेवाले शख्स थे एक दूसरे इंजीनियर विकास भाई जो वाराणसी में रहा करते थे और 1966 में सर्वोदय कार्यकर्ता हो गये थे।
उनकी बात को तो इंजीनियर अनसुना कर नहीं सकता था, लेकिन उसने यह शर्त जरूर रख दी थी कि वह जायेगा जरूर, लेकिन अपनी रिपोर्ट में वह लिखेगा कि वहाँ बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इस पर विकास भाई राजी हो गये। असल में विकास भाई चाहते थे कि कोई हिंदी भाषी इंजीनियर वहाँ जाये, ताकि वहाँ की जमीनी हकीकत का पता चल सके। उनके पास गैर हिंदी भाषी इंजीनियर बहुत थे, लेकिन हिंदी-भाषी इंजीनियरों का टोटा था, इसलिए उस इंजीनियर से उन्होंने सम्पर्क किया था।
उन दिनों बिहार में कानून व्यवस्था लचर थी। खौफ उसके भीतर भी था, लेकिन विकास भाई की बात अनसुनी नहीं कर सका और सहरसा का रुख किया। 8 अक्टूबर यानी बाँध टूटने के करीब एक महीने बाद वह इंजीनियर पहली बार उत्तर बिहार की ज़मीन पर कदम रखता है। कोसी को बेहद करीब से देखता है। लहराती हुई कोसी। इसके बाद वह इंजीनियर विस्थापितों की बची हुई बाँध की झोंपड़ियों में जाकर देखने की कोशिश करता है कि इस विषम परिस्थिति में उनके पास खाने को क्या है, लेकिन अफसोस कि उनके घरों से अन्न का एक दाना नहीं मिलता। उसी वक्त सहसा उसके जेहन में एक सवाल कौंध जाता है कि आखिर इस विषम परिस्थिति में वे क्या खाकर जिंदा रहते होंगे ?
वह इंजीनियर वहाँ कुछ दिन गुजारता है और इस दौरान वह सवाल उसके मन में चलता रहता है। वहाँ से जब वह लौटता है तो उसका मन काम में नहीं लगता है। बस एक ही खयाल से उसका कलेजा लरजने लगता कि तटबंध पर खड़े लोग भूख, ठंड, बीमारी या अन्य कारणों से मर-खप गये होंगे।
सहरसा के दौरे ने उस इंजीनियर के सोचने का नजरिया बदल दिया था कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिये नहीं है। विकास भाई और अन्य बहुत से मित्रों के दबाव में 1985 जून तक सहरसा रुक कर उन्होनें एक राहत कार्य में योगदान दिया। इसी दौरे ने बालू-सीमेंट की गंध से जागने-सोने वाले इंजीनियर में नदियों के प्रति प्रेम भर दिया।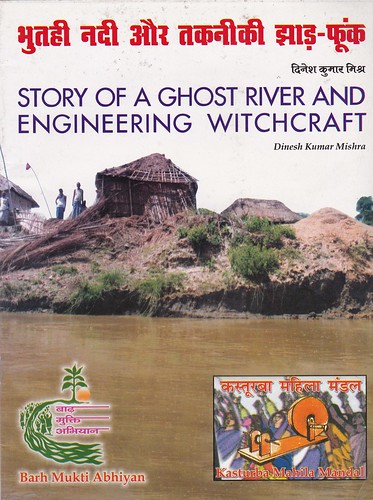 वह इंजीनियर कोई और नहीं दिनेश कुमार मिश्रा थे। सहरसा आने के पहले नदियों से उनका दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कोसी प्रकरण के बाद से उन्होंने नदियों पर बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया। अब तक वह नदियों व बाढ़ पर 10 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। इनमें बाढ़ से त्रस्त-सिंचाई से पस्त, उत्तर बिहार की व्यथा कथा (1990), कोसी- उम्र क़ैद से सजा-ए-मौत तक (1992), बंदिनी महानंदा (1994), बोया पेड़ बबूल का– बाढ़ नियंत्रण का रहस्य (2000), बगावत पर मजबूर मिथिला की कमला नदी (2004), भुतही नदी और तकनीकी झाड़-फूंक (2005), दुई पाटन के बीच में– कोसी नदी की कहानी (2006), बागमती की सद्गति (2010) प्रमुख है। इनमें से अधिकांश पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद भी हुए हैं।
वह इंजीनियर कोई और नहीं दिनेश कुमार मिश्रा थे। सहरसा आने के पहले नदियों से उनका दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कोसी प्रकरण के बाद से उन्होंने नदियों पर बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया। अब तक वह नदियों व बाढ़ पर 10 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। इनमें बाढ़ से त्रस्त-सिंचाई से पस्त, उत्तर बिहार की व्यथा कथा (1990), कोसी- उम्र क़ैद से सजा-ए-मौत तक (1992), बंदिनी महानंदा (1994), बोया पेड़ बबूल का– बाढ़ नियंत्रण का रहस्य (2000), बगावत पर मजबूर मिथिला की कमला नदी (2004), भुतही नदी और तकनीकी झाड़-फूंक (2005), दुई पाटन के बीच में– कोसी नदी की कहानी (2006), बागमती की सद्गति (2010) प्रमुख है। इनमें से अधिकांश पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद भी हुए हैं।
उनकी किताब ‘बोया पेड़ बबूल का’ को वर्ष 2002 में केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के मुद्दे पर बेहतरीन किताब का खिताब दिया था। उसी वर्ष उक्त किताब का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया।दिनेश कुमार मिश्रा का जन्म 22 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में हुआ। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई की और वर्ष 1968 में आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी. टेक और 1970 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री हासिल की। इसके छत्तीस साल बाद यानी 2006 में उन्होंने साउथ गुजरात विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्हें कई फेलोशिप मिल चुके हैं। वह केंद्र सरकार की बाढ़ से सम्बंधित कमेटियों में सदस्य रहे। फिलवक्त वह केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के नमामी गंगे प्रोग्राम के एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य हैं।
हिन्दी और अंग्रेजी के साथ ही वह ओड़िया, बांग्ला व उर्दू भाषा पर भी दखल रखते हैं।
दिनेश कुमार मिश्रा बताते हैं, “मेरी नदियों में उतनी ही रुचि थी जितनी एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को उसके पढ़ाई के समय में होती थी। मेरे गाँव के पास की सबसे नजदीक की नदी तमसा (टौंस) गाँव से 4 किलोमीटर दूर थी। इसलिए नदी के साथ जो स्वाभाविक संपर्क बचपन से होना चाहिए था, वह मुझे कभी मिला ही नहीं। नदियों को देखना अच्छा लगता था और उन्हें प्रणाम कर देना ही मेरे लिये काफी हुआ करता था।”
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रांची में वर्ष 1970 में बिल्डिंग डिजाइन का व्यवसाय शुरू किया। वह धीरे-धीरे बाढ़ में ध्वस्त हुए गाँवों को बसाने की योजना बनाने का भी काम करने लगे थे और इसमें महारत हासिल कर ली। यही महारत उनके सहरसा जाने का कारण बनी।
कोसी की बाढ़ का जायजा लेने के बाद लम्बे समय तक वह ऊहापोह की स्थिति में रहे कि जनसेवा की तरफ रुख करें कि अपने व्यवसाय को चमकाने पर ध्यान दें।
वह कहते हैं, ‘सहरसा में रहते हुए मैं अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पा रहा था जिससे बाज़ार में मेरी साख पर बट्टा लग रहा था। राहत कार्य जुलाई 1985 में समाप्त हुआ और मैं ‘समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य’ (विकास भाई अक्सर यही जुमला उछाल कर उन्हें समाज सेवा के लिये प्ररित किया करते थे) का निर्वाह कर जल्दी अपने काम पर वापस लग जाना चाहता था।”
वह आगे कहते हैं, “राहत कार्य समाप्त होने पर विकास भाई का आग्रह था कि मैं एक रिपोर्ट तैयार कर दूँ कि बाढ़ कैसे आती है और उसका कारण और दुष्प्रभाव क्या-क्या हैं। यह भी कि इसका क्या निराकरण हो सकता है, तो वह फिर मुझे इस तरह का कोई काम करने के लिये दोबारा नहीं कहेंगे। यदि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता, तो मेरे तीन महीने और नष्ट हो जाने वाले थे। मैंने उन्हें बार-बार कहा कि मैं एक इंजीनियर हूँ और जब तक मेरी नाक में सीमेंट या बालू के कण नहीं जाते, तब तक मुझे नींद नहीं आती और इस काम में वह सुविधा नहीं है। उनका कहना था कि वह इसका इंतज़ाम करे देंगे, मगर यह रिपोर्ट समाज के बहुत काम आएगी। इसलिए समाज के हित में मुझे यह काम करना चाहिए। मुझे उनके ‘देश या समाज के हित’ की बात अभी भी समझ में नहीं आती थी। उनके बहुत जोर देने पर मैंने हामी भरी और तीन महीना फिर देश और समाज के हित में बर्बाद करने के लिए तैयार हुआ।” मिश्रा के लिये एक जीप की व्यवस्था कर दी गयी। एक ड्राइवर दे दिया गया और कुछ पैसे भी। तय हुआ कि वह एक महीने तक क्षेत्र में घूमेंगे। दो महीने में एक रिपोर्ट बनाकर देंगे तथा अपने दायित्व से फारिग हो जायेंगे। उन्होंने उत्तर बिहार का दौरा तो किया लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली व उन्हें बैरंग लौट जाना पड़ा।
मिश्रा के लिये एक जीप की व्यवस्था कर दी गयी। एक ड्राइवर दे दिया गया और कुछ पैसे भी। तय हुआ कि वह एक महीने तक क्षेत्र में घूमेंगे। दो महीने में एक रिपोर्ट बनाकर देंगे तथा अपने दायित्व से फारिग हो जायेंगे। उन्होंने उत्तर बिहार का दौरा तो किया लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली व उन्हें बैरंग लौट जाना पड़ा।
इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि नदियों व बाढ़ को लेकर उनको जो सदमा सहरसा में लगा उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिये कोई कुछ बोलने के लिये तैयार न था। उस घटना का उन पर इतना असर जरूर पड़ा था इंजीनियरिंग यदि यही है कि एक झटके में इतने लोग उजड़ जाएँ तो इस खेल को उजागर करना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। यह अलग बात थी कि वह खुद यह काम नहीं करना चाहते थे। वह अभी भी अपने पेशे के प्रति समर्पित थे।
खैर, रिपोर्ट बनाने का काम ठंडे बस्ते में चला गया। सहरसा में अधिक वक्त बिताना उनके व्यवसाय के लिये वाटरलू साबित हो रहा था, सो वह कलकत्ता में कुछ दिनों का कार्यक्रम बना कर अपने बड़े भाई के पास चले गए जो उस समय एक फैक्टरी में जनरल मैनेजर होकर जमशेदपुर से कलकत्ता आ गये थे। लेकिन, नदियाँ तो जैसे उनके पीछे ही पड़ी हुई थीं। एक दिन विकास भाई कलकत्ते में भी आ धमके व रिपोर्ट पर काम करने को कहने लगे। काफी मान-मनौव्वल के बाद मामला बना। उन्हें पहले दौर की बिहार यात्रा में पता लग गया था कि पटना की सिन्हा लाइब्रेरी और कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी में पटना से प्रकाशित होने वाले इंडियन नेशन और सर्चलाइट अखबार की पुरानी फाइलें हैं, जिनसे बिहार में बाढ़ को लेकर उनकी समझ काफी विकसित होगी। विकास भाई ने यह आश्वासन भी दे दिया कि उनकी नाक में सीमेंट व बालू के कण पहुँचाने का भी इंतजाम वह कर देंगे, मतलब उनका व्यवसाय चलता रहे, इसकी व्यवस्था भी वह करेंगे।
उस वक्त नेशनल लाइब्रेरी का समाचार पत्र विभाग कलकत्ते के एसप्लानेड में हुआ करता था। वह बिहार में बाढ़ से सम्बंधित तथ्य जुटाने के लिये करीब सात महीने तक विभिन्न अखबारों, जर्नलों व मैगजीनों की धूल फांकते रहे। इन सात महीनों में उन्होंने वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1985 तक के कालखंड को जी लिया। बाढ़ को लेकर खबरों, खबरों में जिक्र किये गये लोगों के नाम, विधानसभा में बहसों, सरकारी योजनाओं समेत हर तरह की जानकारी इकट्ठी कर ली। इस कालखंड से गुजरते हुए उनके भीतर का ग्रे मैटर जाग उठा था और वह नदियों व बाढ़ पर काम करने के लिये पूरी तरह तैयार हो गये थे। उनके लिये फिर एक जीप और ड्राइवर का इंतज़ाम किया गया और वह फिर उत्तर बिहार की तरफ निकल पड़े।
लम्बे समय तक क्षेत्रों में घूम-घूमकर उन्होंने लोगों से बात की। पटना की लाइब्रेरी से जरूरी तथ्य निकाले व बाढ़ पर अपनी पहली पुस्तक का ड्राफ्ट तैयार किया।
वह थोड़ा मायूस होकर बताते हैं, “अफसोस की बात थी कि जिस दिन मैंने अपनी पुस्तक के पहले ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया, उसी दिन विकास भाई इस दुनिया से कूच कर गये थे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब इस पोथी का मैं क्या करूँ?”
यह 29 दिसंबर 1987 की बात है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वह दोहारे पर आ गये थे क्योंकि उनके गाइड विकास भाई उन्हें अकेला छोड़ गये थे। वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि किताब छपवायें या पूरे मामले को एक सपना समझ कर भूल जायें व अपनी रोजी-रोटी में लग जायें। ‘एक तरफ उसका घर, एक तरफ मयकदा’ जैसी स्थिति के बीच करीब तीन साल बाद यानी 1990 में उनकी पहली किताब ‘बाढ़ से त्रस्त-सिंचाई से पस्त-उत्तर बिहार की व्यथा-कथा’ प्रकाशित हुई। इसका विमोचन उस समय नये-नये मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव ने किया था।
किताब बाजार में आ गयी और विकास भाई को उनका किया हुआ वादा पूरा हो गया, तो फिर एक बार वह दोराहे पर आ गये-एक राह नदियों की तरफ जाती थी व दूसरी राह बिल्डिंग डिजाइनिंग के धंधे की तरफ।
मिश्रा बताते हैं, “मुझे लगा कि एक बार ऑफिस खोल कर बिल्डिंग डिजाइन का काम शुरू किया जाए। मगर, इस बीच मेरा बहुत से लोगों से परिचय हो चुका था और कभी-कभी गोष्ठियों में आने के निमंत्रण भी मिलने लगे थे। लोगों से मुलाक़ातें होतीं, तो वे शिकायत करते कि आपने अपनी किताब में हमारे गाँव या हमारी नदी की चर्चा नहीं की या उसके बारे में बहुत कम लिखा है। हमारी समस्या का कोई ज़िक्र नहीं है आप की किताब में, वगैरह वगैरह। अब मेरे लिये इस समय अहम फैसले का था कि मैं कम से कम उत्तर बिहार की सारी नदियों और उनकी समस्याओं पर पुस्तकें लिखूँ या फिर सबसे क्षमा मांग कर मैदान छोड़ दूँ। मैंने लोगों की अपेक्षा के हक में फैसला किया और तबसे इस काम में लगा हुआ हूँ।” इस फैसले के बाद उन्होंने बिहार की नदियों से जुड़े दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा लिखे किताबों के साथ ही वेद-पुराण भी उन्होंने बांच डाला।
इस फैसले के बाद उन्होंने बिहार की नदियों से जुड़े दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा लिखे किताबों के साथ ही वेद-पुराण भी उन्होंने बांच डाला।
उन्होंने कई बार सरकार को भी मशविरा दिया कि किस तरह बाढ़ की विभीषका रोकी जा सकती है।
वर्ष 2012 में उन्होंने बागमती पर किताब लिखी व इसके बाद फैसला लिया कि गंडक नदी पर एक पुस्तक लिख कर वह अपने काम को विराम देंगे, लेकिन बीच रास्ते बूढ़ी गंडक आ गयी। जैसे कह रही हो कि मैंने क्या बिगाड़ा है कि मुझ पर तुम किताब नहीं लिखोगे। हालाँकि वह तय कर चुके थे कि बूढ़ी गंडक पर एक शब्द भी नहीं लिखेंगे क्योंकि नदियाँ चिर-यौवना होती हैं उन्हें बूढी कहना उनका अपमान करना है, लेकिन नदी की विशेषता ने उनके विचार बदल दिये व उन्होंने चिर-यौवना बूढ़ी गंडक को भी अपने लेखन में शामिल किया।
वह आगे बताते हैं, “दोनों नदियों पर काम करते हुए ख्याल आया कि घाघरा ने मेरा क्या बिगाड़ा है? यह नदी बिहार में गंगा से मिल कर अपना अस्तित्व खो देती है। उसके बारे में न लिखना उसके साथ अन्याय होगा। तब इस पर भी लिखना शुरू किया। तीनों किताबों पर काम चल रहा है।”
उनके लिये यह सब काम करने में नीतिगत दिक्कत इसलिए नहीं आयी, क्योंकि उन्होंने किसी संस्था का गठन न कर अकेले अपने दम पर काम किया। अलबत्ता, किसी संस्था के बैनर तले काम नहीं करने से आर्थिक मोर्चे पर कई बार उनके सामने मुश्किलें आयीं, लेकिन उन्हीं मुश्किलों के बीच राह भी निकल आयी।
उनके अनुसार, संस्था न होने का फायदा भी कम नहीं है। संस्था नहीं होने से मेरा एजेंडा कोई दूसरा तय नहीं करता, मैं करता हूँ और मेरी जवाबदारी सिर्फ मेरे प्रति है। मुझे काम पूरा करने के लिये कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं दिखाता है।
इन दिनों वह कितने सक्रिय हैं? इस सवाल पर वह मीर का एक शेर सुनाते हैं-
जिन जिन को था ये इश्क का आजार मर गए,
अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए।
कहते हैं, जब मैं सहरसा गया था तो मेरी उम्र 38 साल थी और अब 71 साल। अब मेरी उम्र मेरे पक्ष में नहीं है। फिर भी सिर्फ एक ही बात मुझे अपना काम जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करती है, वह यह कि भविष्य में यदि कोई बिहार के पानी, नदी, बाढ़, सिंचाई आदि विषयों पर काम करेगा, तो जो पापड़ मुझे बेलने पड़े, उससे वह मुक्त रहेगा और वो वहाँ से शुरू करेगा, जहाँ मैं समाप्त करूँगा। उसे पीछे झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई पीछे झांकता है, तो उसका एक फायदा होगा कि मैंने क्या-क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था या मुझसे कहाँ-कहाँ चूक हुई, इसका पता लगेगा। ‘देश और समाज के हित में’ मेरे काम का यह मूल्यांकन बहुत उपयोगी होगा।
उनका मानना है कि नदियों को लेकर सरकार का रवैया बेहद उदासीन रहा है व इसका खामियाजा आनेवाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नदियाँ, जंगल, पहाड़ आदि सभी कुछ प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति, जिसे ईश्वर की श्रेष्ठ कृति कहा जाता है, के साथ छेड़-छाड़ की एक मर्यादा है। इसका उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों द्वारा छोटों को आशीर्वाद देते समय यह कहने का रिवाज़ था कि जब तक इस पृथ्वी पर नदियों, जंगलों और पहाड़ों का साम्राज्य रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। दुर्भाग्यवश हम इस परंपरा को भूल गए। इसका इतना लाभ तो था कि नयी पीढ़ी को हमेशा इस बात को याद दिलाया जाता था कि उनके लिये इन जंगलों, पहाड़ों और नदियों का क्या महत्व है। प्रकृति को सीमातीत अतिक्रमण को सहने की आदत नहीं है और वह इसका बदला जरूर लेती है और इसे बर्दाश्त कर पाना सबके बस की बात नहीं है। हमें कम से कम इतना प्रयास तो करना ही चाहिए कि जो संसाधन हमें पूर्वजों से मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी को सुरक्षित करके उन्हें सौंप दें।
दिनेश कुमार मिश्रा जी का पता
डी-29 वसुंधरा इस्टेट, एनएच-33, जमशेदपुर - 831020, झारखंड, मोबाइल नं. +91-9431303360, ई-मेल: dkmishra108@gmail.com












