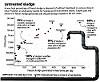Source
जनसत्ता (रविवारी), 13 अक्टूबर 2013
भारत के कई राज्यों में अब भी मैला ढोने की प्रथा जारी है। दो बार कानून बनने और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस दिशा में पूरी सफलता नहीं मिल पाई। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इसे लेकर काफी चिंतित हैं। मामले की पड़ताल कर रही हैं सीत मिश्रा।
सरकार ने तमाम आंदोलन और जनदबाव के बाद 1993 में एक कानून बनाकर सिर पर मैला प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कानून नाकाफी सिद्ध हुआ। इसमें मैला ढोने के तरीकों को स्पष्ट नहीं किया गया था। उसमें केवल शुष्क शौचालयों को शामिल किया गया था। जबकि मैला साफ करने के कई और तरीके हैं, जो बेहद अमानवीय हैं। ओपेन ड्रेन, सेप्टिक टैंक में सफाई, रेलवे ट्रैक पर बिखरे मल को साफ करना, सीवर की सफाई करना वगैरह। 1993 में बने कानून के बेअसर होने की वजह से सरकार एक बार फिर जनदबाव के सामने झुकी। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में भारत एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है तब यह जानना कितना दुखद है कि देश में करीब डेढ़ लाख लोग अब भी सिर पर मैला ढोकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस प्रथा में लगे लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हैं। इस कुप्रथा को बनाए रखने में कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां जिम्मेदार हैं। वैसे तो देश में कई राज्यों ने इस क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है, लेकिन आठ से ज्यादा राज्य अभी भी इस शाप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति हिंदी पट्टी के राज्यों की है। इसमें भी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा लोग मैला प्रथा में लगे हैं। केंद्र सरकार ने निर्मल भारत अभियान के तहत जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शुष्क शौचालय हैं। ये वे आंकड़े हैं जो स्वयं जिला प्रशासन ने सरकार को भेजे हैं। वे आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किए गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,51,367 शुष्क शौचालय हैं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश के सोलह जिलों में व्यापक रूप से यह कुप्रथा जारी है। एक अध्ययन से पता चला है कि मध्य प्रदेश में 506 परिवारों में केवल महिलाएं ही इस काम को करती हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि वाल्मीकि समाज के लोग इस पेशे को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उन्हें इससे अच्छी आय होती है। लेकिन सर्वे में सामने आया है कि एक परिवार मैला उठाने के एवज में इन्हें महज पंद्रह-बीस रुपए रोज़ाना देता है। ऐसे में इन्हें कितना लाभ होता होगा, सोचा जा सकता है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह प्रथा अब भी जहां-तहां कायम है। यह भी कहा जा रहा है कि कई राज्य जानबूझकर अपनी स्थिति छिपा रहे हैं।
सरकार ने तमाम आंदोलन और जनदबाव के बाद 1993 में एक कानून बनाकर सिर पर मैला प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कानून नाकाफी सिद्ध हुआ। इसमें मैला ढोने के तरीकों को स्पष्ट नहीं किया गया था। उसमें केवल शुष्क शौचालयों को शामिल किया गया था। जबकि मैला साफ करने के कई और तरीके हैं, जो बेहद अमानवीय हैं। ओपेन ड्रेन, सेप्टिक टैंक में सफाई, रेलवे ट्रैक पर बिखरे मल को साफ करना, सीवर की सफाई करना वगैरह। 1993 में बने कानून के बेअसर होने की वजह से सरकार एक बार फिर जनदबाव के सामने झुकी। आखिरकार 2012 में मैला प्रथा निषेध पुनर्वास विधेयक को संसद ने पारित किया। इस कानून में कुछ हद तक पुरानी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। हालांकि, इसके आलोचक अभी भी इसे नाकाफी मानते हैं।
इस मामले का उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया। अक्टूबर 2007 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2004 में एक जनहित याचिका पर मैला प्रथा निषेध अधिनियम को सख़्ती से लागू करने का आदेश दिया था। सारी कोशिशें नाकाफी रहीं।
इस प्रथा में जुते परिवारों के सामने कई कठिनाइयाँ हैं। असल समस्या पुनर्वास की है। इस प्रथा को छोड़ने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। यह स्थिति कुछ-कुछ बाल मजदूरी प्रथा जैसी है। अक्सर बाल मज़दूरों को उनके काम से हटा तो दिया जाता है, लेकिन विकल्प के अभाव में वे घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाते हैं यही हाल इस प्रथा में लगे लोगों का है। कुछ राज्यों में तो यह भी देखने आया कि जो परिवार इसमें लगे होते हैं वे इसे जागीर कहते हैं। यह एक तरह का खानदानी काम है।
 अगर हम इस प्रथा के तहों के खोजें तो पाएंगे कि दूसरी तमाम बुराइयों की तरह जाति प्रथा इसके भी जड़ में हैं। कुछ काम निम्न मानी जाने वाली जातियों को सौंप दिया गया, जिसे वे चाहे-अनचाहे सदियों से ढोती आ रही हैं। यों कहिए कि इन कामों को उनके अस्तित्व से जोड़ दिया गया। जब समाज को जाति व्यवस्था में बांटा गया तो सबसे निचले पायदान पर दलितों को स्थान मिला और उन्हें सबकी सेवा का ज़िम्मा सौंपा गया। प्राचीन समय से ही दूसरे लोगों का मैला उठाने का काम दलित जाति के लोग, जिनमें महिलाएं ज्यादा हैं, कर रही हैं।
अगर हम इस प्रथा के तहों के खोजें तो पाएंगे कि दूसरी तमाम बुराइयों की तरह जाति प्रथा इसके भी जड़ में हैं। कुछ काम निम्न मानी जाने वाली जातियों को सौंप दिया गया, जिसे वे चाहे-अनचाहे सदियों से ढोती आ रही हैं। यों कहिए कि इन कामों को उनके अस्तित्व से जोड़ दिया गया। जब समाज को जाति व्यवस्था में बांटा गया तो सबसे निचले पायदान पर दलितों को स्थान मिला और उन्हें सबकी सेवा का ज़िम्मा सौंपा गया। प्राचीन समय से ही दूसरे लोगों का मैला उठाने का काम दलित जाति के लोग, जिनमें महिलाएं ज्यादा हैं, कर रही हैं।
इस प्रथा के विरोध में समय-समय पर आवाजें भी उठीं। कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन असल सवाल तो इसके पूरी तरह खात्मे को लेकर है। सफाई कर्मचारी आंदोलन पिछले कई सालों से इसके उन्मूलन के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। यह अभियान भारतीय समाज को बेहतर बनाने के लिए उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है जहां एक शख्स की पहचान दूसरे शख्स के अपशिष्ट उठाने के तौर पर मौजूद है। पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करके इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिला। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने और इसमें लगे लोगों को रोज़गार देने और शुष्क शौचालयों को (जिनमें फ्लश की व्यवस्था नहीं होती) बदलने के लिए 460 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। लेकिन खर्च मात्र 146.04 करोड़ ही किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 तक मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का दावा किया गया।
मैला प्रथा उन्मूलन और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1990 में कुछ कदम उठाए थे। उस समय इसे जड़ से मिटाने के लिए 1995 तक की समय सीमा तय की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 1998 कर दिया गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वे 2000 तक इस प्रथा को जड़ से खत्म कर देगें। समय खिसकता रहा और कुप्रथा जारी रही। सर्वेक्षण में पाया गया कि इस काम में लगे परिवारों को समाज में भी काफी दंश झेलना पड़ता है। अस्वच्छ कामों में लगी महिलाओं को किसी कला या अन्य कार्य-कौशल के लिए छह माह का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। उसे सरकारें ठीक से लागू नहीं करतीं। मध्य प्रदेश के छह जिलों से करीब छह सौ महिलाओं को इस पेशे से मुक्त कराया लेकिन बाद में तीस महिलाओं ने इस पेशे को दोबारा अपना लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां इन महिलाओं ने मैला ढोने से इनकार कर अपने लिए नया रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विफलता हाथ लगी। महाराष्ट्र की सुमित्रा बाई ने खुद को इस पेशे के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए कोशिश की। उन्हें वैकल्पिक रोज़गार के लिए बीस हजार रुपए का ऋण भी मिला। वह खुश थी कि अब वह समाज में बेहतर और सम्माननीय जीवन जी सकेगी, उसके बच्चों को कभी इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा सुमित्रा बाई ने ऋण के पैसों से एक कपड़े की दुकान तो खोल ली, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी उनकी दुकान पर कोई नहीं आया। मजबूरन उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और समाज की बनाई कुरीतियों की चक्की में पिसने के लिए दोबारा वापस लौटना पड़ा।
यह सम्मान और गरिमा का प्रश्न है। लिहाजा आर्थिक मदद या सरकारी योजना इसका जवाब नहीं ढूंढ़ सकती। सरकार मानती हैं कि मैला ढोने का काम छोड़ने पर उन्हें दूसरे अच्छे काम मिल जाते हैं,जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा करने पर उनके दूसरे विकल्प भी छिन जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले की मैला ढोने का काम छोड़ चुकी शांति बाई का कहना है कि हमें इस काम के एवज में हर घर से एक बासी रोटी और त्योहारों पर पुराने कपड़े मिलते थे। वे हमें अपना गुलाम मानते थे, इसलिए काम करवाने के बदले हमारी कुछ मदद भी कर देते थे। लेकिन जब से यह का छोड़ा है तब से हमारा तो जैसे सामाजिक बहिष्कार हो गया है। अब जरूरत पड़ने पर जब हम सवर्णों से रोटी या अन्य मदद मांगने जाते हैं तो एक भी परिवार हमारी मदद नहीं करता। ऐसे ही, देवास के गंधर्वपुरी गांव की मुन्नीबाई से कहा गया कि जिन्होंने तुमसे मैला ढोने का काम छुड़वाया है अब उन्हीं से जाकर मदद मांगों। जब इस तरह की विषम परिस्थितियां सामने आती हैं, रोटी के लाले पड़ जाते हैं, घर में बच्चे भूख से कुलबुलाते हैं, तो आत्मसम्मान और गरिमा की सुध नहीं रहती। फिर तो बस दो जून की रोटी के इंतज़ाम का खयाल ही दिमाग में आ सकता है और उसकी व्यवस्था के लिए महिलाएं जिस दलदल से बमुश्किल निकली होती हैं दोबारा उसी ओर रुख कर लेती हैं। हालांकि असभ्य समाज में इसका चलन जोरों पर नहीं था, लेकिन सभ्य होता समाज दबे-कुचले लोगों के लिए क्रुर रवैया अपनाता है।
 यह इस पेशे को अपनाने या छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के भेदवादी चरित्र को चुनौती दने का मसला है। मैला ढोने की प्रथा एक तरह से जाति व्यवस्था और पुरुषों द्वारा इन महिलाओं पर थोपी गई हिंसा है। कानूनन शुष्क शौचालय को इंसान से साफ करवाना प्रतिबंधित है और अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई शुष्क शौचालय मालिक इस कार्य को किसी सफाई कर्मचारी से कराता है तो यह कार्य दंडनीय है। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि हरियाणा के दो जिलों को छोड़कर अभी तक किसी भी शुष्क शौचालय मालिक को इस अधिनियम के तहत सजा नहीं मिली।
यह इस पेशे को अपनाने या छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के भेदवादी चरित्र को चुनौती दने का मसला है। मैला ढोने की प्रथा एक तरह से जाति व्यवस्था और पुरुषों द्वारा इन महिलाओं पर थोपी गई हिंसा है। कानूनन शुष्क शौचालय को इंसान से साफ करवाना प्रतिबंधित है और अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई शुष्क शौचालय मालिक इस कार्य को किसी सफाई कर्मचारी से कराता है तो यह कार्य दंडनीय है। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि हरियाणा के दो जिलों को छोड़कर अभी तक किसी भी शुष्क शौचालय मालिक को इस अधिनियम के तहत सजा नहीं मिली।
इस प्रथा को लेकर कई बार विचारकों के बीच तीखे मतभेद भी देखे गए। गांधीजी ने कहा था, ‘बच्चों का मलमूत्र तो माता-पिता साफ करते हैं, यह तो पुण्य का काम है। इस कार्य में लगे लोगों को यह पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कामना की थी, ‘मेरा अगला जन्म भंगी के घर हो इस बात पर भीमराव अंबेडकर ने तुर्की-ब-तुर्की कहा था, ‘गांधी को अगला जन्म लेने की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए, वे इसी जन्म में यह काम कर सकते हैं। हमने बहुत पुण्य कमा लिया, अब गांधीजी अपने अनुयायियों को यह कार्य कराकर पुण्य और लाभ दोनों कमाएं।’
मैला प्रथा में लगी महिलाओं की त्रासदी देखनी हो तो भाषा सिंह की हाल में प्रकाशित किताब ‘अदृश्य भारत’ को देखना चाहिए। उन्होंने एक जगह लिखा है, ‘35 साल की मुसरी वासफो ने हाथ डब्बू बाल्टी में डालते हुए व्यंग्य से कहा- कैमरा संभालों, छिंटा न पड़े, नीचे बैठकर फोटो मत लो और न ज्यादा पास आओ, वरना कढ़ी और दाल छूट जाएगी। पेट उछलने लगा...। भयानक गंध से बजबजाते गटर जैसे जंक्शन पर तो जब उन महिलाओं को बाल्टियां पलटते देख रही थी,तो वाकई कैमरा हाथ से फिसल ही गया, सिर घूम गया और बस, जाति की गंधाती सच्चाई पर चीखने का मन हुआ।’
यह कुप्रथा समाज के साथ ही देश की सभ्यता और तरक्की पर बदनुमा दाग की तरह है। महज कानून बना देने से काम नहीं बनने वाला।
एक तरफ तरक्की की चौंधिया देने वाली रोशनी है तो दूसरी ओर एक दूसरी दुनिया बसी है जहां सिर्फ बजबजाता घनघोर अंधेरा है।
सरकार ने तमाम आंदोलन और जनदबाव के बाद 1993 में एक कानून बनाकर सिर पर मैला प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कानून नाकाफी सिद्ध हुआ। इसमें मैला ढोने के तरीकों को स्पष्ट नहीं किया गया था। उसमें केवल शुष्क शौचालयों को शामिल किया गया था। जबकि मैला साफ करने के कई और तरीके हैं, जो बेहद अमानवीय हैं। ओपेन ड्रेन, सेप्टिक टैंक में सफाई, रेलवे ट्रैक पर बिखरे मल को साफ करना, सीवर की सफाई करना वगैरह। 1993 में बने कानून के बेअसर होने की वजह से सरकार एक बार फिर जनदबाव के सामने झुकी। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में भारत एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है तब यह जानना कितना दुखद है कि देश में करीब डेढ़ लाख लोग अब भी सिर पर मैला ढोकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस प्रथा में लगे लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हैं। इस कुप्रथा को बनाए रखने में कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां जिम्मेदार हैं। वैसे तो देश में कई राज्यों ने इस क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है, लेकिन आठ से ज्यादा राज्य अभी भी इस शाप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति हिंदी पट्टी के राज्यों की है। इसमें भी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा लोग मैला प्रथा में लगे हैं। केंद्र सरकार ने निर्मल भारत अभियान के तहत जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शुष्क शौचालय हैं। ये वे आंकड़े हैं जो स्वयं जिला प्रशासन ने सरकार को भेजे हैं। वे आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किए गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,51,367 शुष्क शौचालय हैं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश के सोलह जिलों में व्यापक रूप से यह कुप्रथा जारी है। एक अध्ययन से पता चला है कि मध्य प्रदेश में 506 परिवारों में केवल महिलाएं ही इस काम को करती हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि वाल्मीकि समाज के लोग इस पेशे को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उन्हें इससे अच्छी आय होती है। लेकिन सर्वे में सामने आया है कि एक परिवार मैला उठाने के एवज में इन्हें महज पंद्रह-बीस रुपए रोज़ाना देता है। ऐसे में इन्हें कितना लाभ होता होगा, सोचा जा सकता है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह प्रथा अब भी जहां-तहां कायम है। यह भी कहा जा रहा है कि कई राज्य जानबूझकर अपनी स्थिति छिपा रहे हैं।
सरकार ने तमाम आंदोलन और जनदबाव के बाद 1993 में एक कानून बनाकर सिर पर मैला प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कानून नाकाफी सिद्ध हुआ। इसमें मैला ढोने के तरीकों को स्पष्ट नहीं किया गया था। उसमें केवल शुष्क शौचालयों को शामिल किया गया था। जबकि मैला साफ करने के कई और तरीके हैं, जो बेहद अमानवीय हैं। ओपेन ड्रेन, सेप्टिक टैंक में सफाई, रेलवे ट्रैक पर बिखरे मल को साफ करना, सीवर की सफाई करना वगैरह। 1993 में बने कानून के बेअसर होने की वजह से सरकार एक बार फिर जनदबाव के सामने झुकी। आखिरकार 2012 में मैला प्रथा निषेध पुनर्वास विधेयक को संसद ने पारित किया। इस कानून में कुछ हद तक पुरानी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। हालांकि, इसके आलोचक अभी भी इसे नाकाफी मानते हैं।
इस मामले का उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया। अक्टूबर 2007 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2004 में एक जनहित याचिका पर मैला प्रथा निषेध अधिनियम को सख़्ती से लागू करने का आदेश दिया था। सारी कोशिशें नाकाफी रहीं।
इस प्रथा में जुते परिवारों के सामने कई कठिनाइयाँ हैं। असल समस्या पुनर्वास की है। इस प्रथा को छोड़ने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। यह स्थिति कुछ-कुछ बाल मजदूरी प्रथा जैसी है। अक्सर बाल मज़दूरों को उनके काम से हटा तो दिया जाता है, लेकिन विकल्प के अभाव में वे घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाते हैं यही हाल इस प्रथा में लगे लोगों का है। कुछ राज्यों में तो यह भी देखने आया कि जो परिवार इसमें लगे होते हैं वे इसे जागीर कहते हैं। यह एक तरह का खानदानी काम है।
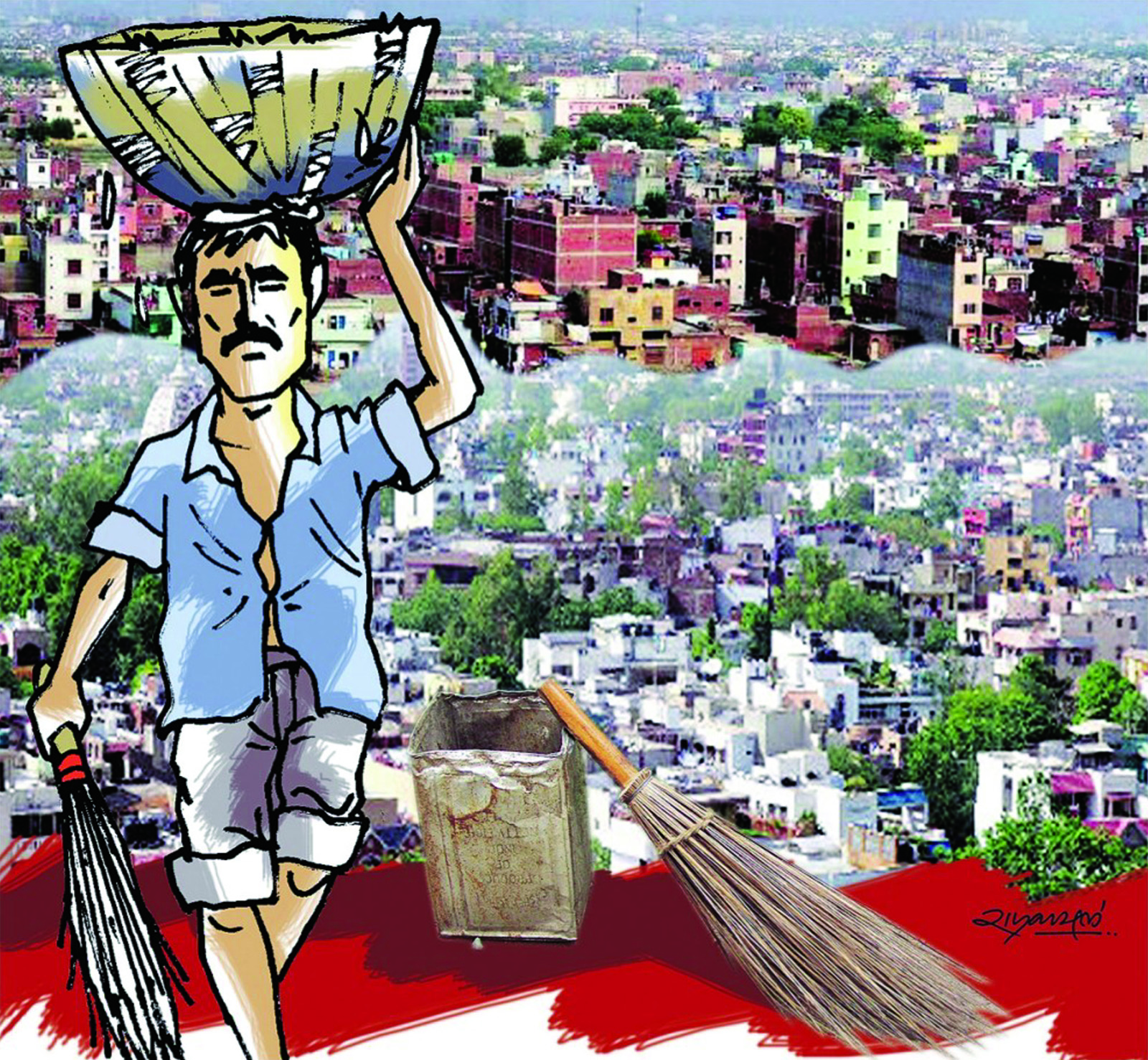 अगर हम इस प्रथा के तहों के खोजें तो पाएंगे कि दूसरी तमाम बुराइयों की तरह जाति प्रथा इसके भी जड़ में हैं। कुछ काम निम्न मानी जाने वाली जातियों को सौंप दिया गया, जिसे वे चाहे-अनचाहे सदियों से ढोती आ रही हैं। यों कहिए कि इन कामों को उनके अस्तित्व से जोड़ दिया गया। जब समाज को जाति व्यवस्था में बांटा गया तो सबसे निचले पायदान पर दलितों को स्थान मिला और उन्हें सबकी सेवा का ज़िम्मा सौंपा गया। प्राचीन समय से ही दूसरे लोगों का मैला उठाने का काम दलित जाति के लोग, जिनमें महिलाएं ज्यादा हैं, कर रही हैं।
अगर हम इस प्रथा के तहों के खोजें तो पाएंगे कि दूसरी तमाम बुराइयों की तरह जाति प्रथा इसके भी जड़ में हैं। कुछ काम निम्न मानी जाने वाली जातियों को सौंप दिया गया, जिसे वे चाहे-अनचाहे सदियों से ढोती आ रही हैं। यों कहिए कि इन कामों को उनके अस्तित्व से जोड़ दिया गया। जब समाज को जाति व्यवस्था में बांटा गया तो सबसे निचले पायदान पर दलितों को स्थान मिला और उन्हें सबकी सेवा का ज़िम्मा सौंपा गया। प्राचीन समय से ही दूसरे लोगों का मैला उठाने का काम दलित जाति के लोग, जिनमें महिलाएं ज्यादा हैं, कर रही हैं।इस प्रथा के विरोध में समय-समय पर आवाजें भी उठीं। कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन असल सवाल तो इसके पूरी तरह खात्मे को लेकर है। सफाई कर्मचारी आंदोलन पिछले कई सालों से इसके उन्मूलन के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। यह अभियान भारतीय समाज को बेहतर बनाने के लिए उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है जहां एक शख्स की पहचान दूसरे शख्स के अपशिष्ट उठाने के तौर पर मौजूद है। पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करके इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिला। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने और इसमें लगे लोगों को रोज़गार देने और शुष्क शौचालयों को (जिनमें फ्लश की व्यवस्था नहीं होती) बदलने के लिए 460 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। लेकिन खर्च मात्र 146.04 करोड़ ही किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 तक मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का दावा किया गया।
मैला प्रथा उन्मूलन और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1990 में कुछ कदम उठाए थे। उस समय इसे जड़ से मिटाने के लिए 1995 तक की समय सीमा तय की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 1998 कर दिया गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वे 2000 तक इस प्रथा को जड़ से खत्म कर देगें। समय खिसकता रहा और कुप्रथा जारी रही। सर्वेक्षण में पाया गया कि इस काम में लगे परिवारों को समाज में भी काफी दंश झेलना पड़ता है। अस्वच्छ कामों में लगी महिलाओं को किसी कला या अन्य कार्य-कौशल के लिए छह माह का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। उसे सरकारें ठीक से लागू नहीं करतीं। मध्य प्रदेश के छह जिलों से करीब छह सौ महिलाओं को इस पेशे से मुक्त कराया लेकिन बाद में तीस महिलाओं ने इस पेशे को दोबारा अपना लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां इन महिलाओं ने मैला ढोने से इनकार कर अपने लिए नया रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विफलता हाथ लगी। महाराष्ट्र की सुमित्रा बाई ने खुद को इस पेशे के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए कोशिश की। उन्हें वैकल्पिक रोज़गार के लिए बीस हजार रुपए का ऋण भी मिला। वह खुश थी कि अब वह समाज में बेहतर और सम्माननीय जीवन जी सकेगी, उसके बच्चों को कभी इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा सुमित्रा बाई ने ऋण के पैसों से एक कपड़े की दुकान तो खोल ली, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी उनकी दुकान पर कोई नहीं आया। मजबूरन उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और समाज की बनाई कुरीतियों की चक्की में पिसने के लिए दोबारा वापस लौटना पड़ा।
यह सम्मान और गरिमा का प्रश्न है। लिहाजा आर्थिक मदद या सरकारी योजना इसका जवाब नहीं ढूंढ़ सकती। सरकार मानती हैं कि मैला ढोने का काम छोड़ने पर उन्हें दूसरे अच्छे काम मिल जाते हैं,जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा करने पर उनके दूसरे विकल्प भी छिन जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले की मैला ढोने का काम छोड़ चुकी शांति बाई का कहना है कि हमें इस काम के एवज में हर घर से एक बासी रोटी और त्योहारों पर पुराने कपड़े मिलते थे। वे हमें अपना गुलाम मानते थे, इसलिए काम करवाने के बदले हमारी कुछ मदद भी कर देते थे। लेकिन जब से यह का छोड़ा है तब से हमारा तो जैसे सामाजिक बहिष्कार हो गया है। अब जरूरत पड़ने पर जब हम सवर्णों से रोटी या अन्य मदद मांगने जाते हैं तो एक भी परिवार हमारी मदद नहीं करता। ऐसे ही, देवास के गंधर्वपुरी गांव की मुन्नीबाई से कहा गया कि जिन्होंने तुमसे मैला ढोने का काम छुड़वाया है अब उन्हीं से जाकर मदद मांगों। जब इस तरह की विषम परिस्थितियां सामने आती हैं, रोटी के लाले पड़ जाते हैं, घर में बच्चे भूख से कुलबुलाते हैं, तो आत्मसम्मान और गरिमा की सुध नहीं रहती। फिर तो बस दो जून की रोटी के इंतज़ाम का खयाल ही दिमाग में आ सकता है और उसकी व्यवस्था के लिए महिलाएं जिस दलदल से बमुश्किल निकली होती हैं दोबारा उसी ओर रुख कर लेती हैं। हालांकि असभ्य समाज में इसका चलन जोरों पर नहीं था, लेकिन सभ्य होता समाज दबे-कुचले लोगों के लिए क्रुर रवैया अपनाता है।
 यह इस पेशे को अपनाने या छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के भेदवादी चरित्र को चुनौती दने का मसला है। मैला ढोने की प्रथा एक तरह से जाति व्यवस्था और पुरुषों द्वारा इन महिलाओं पर थोपी गई हिंसा है। कानूनन शुष्क शौचालय को इंसान से साफ करवाना प्रतिबंधित है और अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई शुष्क शौचालय मालिक इस कार्य को किसी सफाई कर्मचारी से कराता है तो यह कार्य दंडनीय है। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि हरियाणा के दो जिलों को छोड़कर अभी तक किसी भी शुष्क शौचालय मालिक को इस अधिनियम के तहत सजा नहीं मिली।
यह इस पेशे को अपनाने या छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के भेदवादी चरित्र को चुनौती दने का मसला है। मैला ढोने की प्रथा एक तरह से जाति व्यवस्था और पुरुषों द्वारा इन महिलाओं पर थोपी गई हिंसा है। कानूनन शुष्क शौचालय को इंसान से साफ करवाना प्रतिबंधित है और अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई शुष्क शौचालय मालिक इस कार्य को किसी सफाई कर्मचारी से कराता है तो यह कार्य दंडनीय है। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि हरियाणा के दो जिलों को छोड़कर अभी तक किसी भी शुष्क शौचालय मालिक को इस अधिनियम के तहत सजा नहीं मिली।इस प्रथा को लेकर कई बार विचारकों के बीच तीखे मतभेद भी देखे गए। गांधीजी ने कहा था, ‘बच्चों का मलमूत्र तो माता-पिता साफ करते हैं, यह तो पुण्य का काम है। इस कार्य में लगे लोगों को यह पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कामना की थी, ‘मेरा अगला जन्म भंगी के घर हो इस बात पर भीमराव अंबेडकर ने तुर्की-ब-तुर्की कहा था, ‘गांधी को अगला जन्म लेने की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए, वे इसी जन्म में यह काम कर सकते हैं। हमने बहुत पुण्य कमा लिया, अब गांधीजी अपने अनुयायियों को यह कार्य कराकर पुण्य और लाभ दोनों कमाएं।’
मैला प्रथा में लगी महिलाओं की त्रासदी देखनी हो तो भाषा सिंह की हाल में प्रकाशित किताब ‘अदृश्य भारत’ को देखना चाहिए। उन्होंने एक जगह लिखा है, ‘35 साल की मुसरी वासफो ने हाथ डब्बू बाल्टी में डालते हुए व्यंग्य से कहा- कैमरा संभालों, छिंटा न पड़े, नीचे बैठकर फोटो मत लो और न ज्यादा पास आओ, वरना कढ़ी और दाल छूट जाएगी। पेट उछलने लगा...। भयानक गंध से बजबजाते गटर जैसे जंक्शन पर तो जब उन महिलाओं को बाल्टियां पलटते देख रही थी,तो वाकई कैमरा हाथ से फिसल ही गया, सिर घूम गया और बस, जाति की गंधाती सच्चाई पर चीखने का मन हुआ।’
यह कुप्रथा समाज के साथ ही देश की सभ्यता और तरक्की पर बदनुमा दाग की तरह है। महज कानून बना देने से काम नहीं बनने वाला।
एक तरफ तरक्की की चौंधिया देने वाली रोशनी है तो दूसरी ओर एक दूसरी दुनिया बसी है जहां सिर्फ बजबजाता घनघोर अंधेरा है।