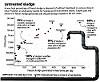लेखक
स्वच्छता दिवस, 02 अक्टूबर 2015 पर विशेष
 देश में साफ-सफाई के लिये नई सरकार का नए सिरे से अभियान का नारा लगाए जाने को एक साल होने आ रहा है। पिछले साल दो अक्टूबर को लगाए गए इस नारे के बाद क्या-क्या हुआ इसका कोई व्यवस्थित लेखा-जोखा नहीं मिलता। लेकिन जब-जब इस अभियान के लिये ब्रांड अम्बेसडरों का एलान होता है या नए नेता झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हैं तो अहसास होता है कि नारा जिन्दा है।
देश में साफ-सफाई के लिये नई सरकार का नए सिरे से अभियान का नारा लगाए जाने को एक साल होने आ रहा है। पिछले साल दो अक्टूबर को लगाए गए इस नारे के बाद क्या-क्या हुआ इसका कोई व्यवस्थित लेखा-जोखा नहीं मिलता। लेकिन जब-जब इस अभियान के लिये ब्रांड अम्बेसडरों का एलान होता है या नए नेता झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हैं तो अहसास होता है कि नारा जिन्दा है।सोचा गया होगा कि साफ-सफाई को लेकर देश के स्तर पर प्रचार की कमी है यानी जागरुकता की कमी है सो यह प्रचार अभियान जोर-शोर से चलाने का एलान किया गया होगा। यह एक तथ्य है कि गुलामी के दो सौ साल बाद आजाद हुए देश को चौतरफा अशिक्षा, कुपोषण और गरीबी विरासत में मिली थी।
आजाादी के समय 36 करोड़ आबादी वाले देश में सिलसिला बैठाते हुए 68 साल में जो कुछ हुआ उसे एक नजर में देखना या दिखाना उतना आसान नहीं है। हाँ आज एक सौ तीस करोड़ अबादी वाले देश में यह कह देना जरूर आसान था कि आजादी के बाद ढंग से नियोजन यानी प्लानिंग का काम नहीं हुआ। सो सभी कामों के नए सिरे से एलानों का होना स्वाभाविक था।
शायद इसी हिसाब से देश को चमचमाता हुआ बनाने या दिखाने के लिये स्वच्छता अभियान का नारा चलाने की बात नए लोगों के दिमाग में आई होगी। और हो सकता है कि नई सरकार आने के बाद यह भी सोचा गया हो कि कालाधन, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी के मामले में कुछ कर दिखाना आसान नहीं है लिहाजा कुछ कर दिखाने लायक आसान काम भी पकड़ लिये जाएँ।
बहुत सम्भव है कि कुछ प्रबन्धन पटु योजनाकारों ने सोचा हो कि स्वच्छता अभियान का नारा चलाना इसलिये आसान होगा क्योंकि सफाई का मामला आम आदमी की जरूरत, चाह और इच्छा से जुड़ा मुद्दा है लिहाजा आम आदमी ऐसे लक्ष्य को सुनकर ही गदगद हो जाएगा। इस आसान से दिखने वाले काम का तीसरा लक्षण यह भी कि फिलहाल आम लोगों के सहयोग से चलाने के इरादे के कारण इस काम के लिये सरकार को किसी भारी-भरकम खर्च का इन्तजाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहरहाल यह नारा बनाया गया। प्रचार के लिये देश की सेलिब्रिटी की भारी-भरकम फौज लगाई गई। लेकिन सामान्य अनुभव यह रहा कि पूरा एक साल बीतने के बावजूद इस अभियान का कोई असर नहीं दिख रहा है। ऊपर से एक बड़ी भारी चक्कलस यह और खड़ी हो गई है कि देश भर की नगर पालिकाओं और नगर निगमों से पैदा होने वाली गन्दगी और बदबूदार कूड़ा शहर से उठाकर जिन गाँवों में डाला जा रहा है उन गाँव वालों को लगने लगा है कि नए सफाई अभियान का सारा खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
इसका एक सनसनीखेज उदाहरण इस पत्रकार को 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस पर सागर के इंक मीडिया पत्रकारिता संस्थान में आयोजित कार्यशाला के दौरान मिला। कार्यशाला के बाद चर्चा के दौरान पत्रकारिता में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे मेधावी प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के सागर नगर निगम के स्वच्छता अभियान के काम का लेखा-जोखा बनाने के काम पर उन्हें लगाया गया था। इसकी रिपोर्ट बनाने के लिये उन्होंने बाहर निकल कर यह भी देखा कि मध्य प्रदेश के सागर शहर से हर दिन उठाए जा रहे सैंकड़ों टन गन्दे और बदबूदार कूड़े कचरे का निस्तारण और प्रबन्धन कैसे किया जाता है।
पत्रकारिता के प्रशिक्षु पता करते-करते सागर शहर की सीमा से बाहर उस गाँव हफसिली तक पहुँच गए जहाँ नगरनिगम की गन्दगी फेंकी जाती है। गाँव में चारों तरफ असहनीय बदबू, घर-घर मक्खियाँ और मच्छर और स्वभावतः गरीब गाँव में घर-घर बीमारियों से परेशान गाँव वालों ने इन भावी पत्रकारों के सामने अपना रोना रोया। पत्रकारिता के प्रशिक्षुओं ने सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की। इन भावी पत्रकारों ने गाँव में बना दिये गए जुगुप्सा और घिनौनेपन के भयावह हालात की तस्वीरें भी लीं।
 तर्क, विश्वसनीयता, करुणा सनसनी चारों तत्त्वों से मिलकर बनी यह वहाँ कहाँ जर्नलिस्टिक रिपोर्ट किसी अखबार या मैगज़ीन में छप नहीं पाई है। हो सकता है कि ऐसा इसलिये हुआ हो क्योंकि यह प्राणांतक समस्या गाँव की है। वहाँ आमतौर पर अखबार बिकते नहीं है। इसलिये अखबार या टीवी चैनलों की व्यवस्था में गाँव की काई बीट भी नहीं बन पाई है। और फिर नई सरकार के किसी भी नारे या अभियान और खासतौर पर स्वच्छता अभियान से जुड़ी कोई भी खराब बात बाहर निकले इसे शायद मीडिया में फिलहाल अच्छा नहीं माना जा रहा है। खैर।
तर्क, विश्वसनीयता, करुणा सनसनी चारों तत्त्वों से मिलकर बनी यह वहाँ कहाँ जर्नलिस्टिक रिपोर्ट किसी अखबार या मैगज़ीन में छप नहीं पाई है। हो सकता है कि ऐसा इसलिये हुआ हो क्योंकि यह प्राणांतक समस्या गाँव की है। वहाँ आमतौर पर अखबार बिकते नहीं है। इसलिये अखबार या टीवी चैनलों की व्यवस्था में गाँव की काई बीट भी नहीं बन पाई है। और फिर नई सरकार के किसी भी नारे या अभियान और खासतौर पर स्वच्छता अभियान से जुड़ी कोई भी खराब बात बाहर निकले इसे शायद मीडिया में फिलहाल अच्छा नहीं माना जा रहा है। खैर।हफसिली के इस मामले से यह समझ लेना ठीक नहीं होगा कि मौजूदा स्वच्छता अभियान से सिर्फ गाँवों पर आफत आ गई है। सफाई के मामले में शहर किसी कम नर्क से नहीं जूझ रहे हैं। शहरी इलाके से गन्दगी उठाने के काम का व्यवस्थित लेखा-जोखा अभी नहीं बन पाया है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव है कि हर गली मुहल्ले के बाहर कूड़े कचरे के ढेर जमा हैं।
बात निकली तो पता चला कि शहर से उठाई जा रही गन्दगी को ठिकाने लगाने की समस्या सार्वभौमिक है। मसलन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाज़ियाबाद नगर निगम ने अपनी शहरी गन्दगी बाहर फेंकने के लिये डूंडाहेड़ा गाँव में पाँच एकड़ जमीन का इन्तजाम किया था। इस गाँव में बदबू, मक्खियों और मच्छरों के मारे ऐसा नर्क बन गया कि गाँववालों का जीना दूभर हो गया। परेशान गाँव ने एकजुट होकर जबरदस्त विरोध किया। इस समय क्या स्थिति है इसका पता तो नहीं चलता लेकिन गाजियाबाद शहर में जहाँ-तहाँ कूड़े के ढ़ेर बढ़ना शुरू हो गए हैं।
गाजियाबाद के सबसे आलीशान इलाके भारत सरकार के सीजीओ कॉपलेक्स में फार्माकोपिया प्रयोगशालाओं के बाहर इतना कूड़ा बिखरा पड़ा रहने लगा है जैसे शहर की गन्दगी को ठिकाने लगाने का अड्डा यही हो। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहरी इलाकों की गन्दगी को ठिकाने लगाने की कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
इतनी बड़ी समस्या कि शहरी इलाकों में सदियों से बने तालाब और झीलें कूड़े से पटकर सपाट हो रही हैं। उप्र के झाँसी जिले के एक बड़े कस्बे मउरानीपुर में तो यह आलम है कि शहर के सारे गन्दे नाले नदी में गिरते ही थे अब ठोस कचरा भी नदी में डाला जाता हुआ देखा जा सकता है। साल दो साल पहले तक पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएँ जल और भूजल प्रदूषण को लेकर अभियान चलाती दिखती थीं वे भी गायब सी दिख रही हैं।
पीछे पलट कर देखें तो अस्सी के दशक के बाद हर क्षेत्र में प्रबन्धन कौशल के इस्तेमाल का जो युग शुरू हुआ था उस युग की शुरूआत में ही परम्परावादी विद्वान तबके ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तीस साल पहले के माहौल को पीछे मुड़कर देखें तो पर्यावरण को लेकर देश में चिन्ता शुरू हो गई थी।
बड़ी आसानी से याद आ जाता है कि पूरे देश में चारों तरफ पॉलीथिन की थैलियों की भरमार से पर्यावरण कार्यकर्ता चिन्तित हो उठे थे। उसी समय से ठोस कचरे के प्रबन्धन के उपायों पर सोचना शुरू हो गया था। लेकिन जब हिसाब लगा कि हर घर से साग-सब्जियों और फलों के छिलके, दूध, दही, मक्खन के प्लास्टिक के कप और पैकेट, रेडीमेड नमकीन की पॉलीथिन की थैलियाँ और रसोई से निकली जूठन, चाय की पत्ती वगैरह का वजन आधा किलोग्राम प्रतिदिन होता है।
इस ठोस कचरे का स्वीकार्य पूरी तरह से निस्तारण या प्रबन्धन इतना खर्चीला काम है कि देश का पूरा बजट ही कम पड़ जाये। मसलन इस कचरे की रीसाइकिलिंग या पुर्नचक्रण जैसे उपाय हमें अपनी हैसियत से परे दिखने लगे थे। सिर्फ दो लाख आबादी के नगर या कस्बे से रोज़ाना निकलने वाले कम-से-कम एक लाख किलोग्राम कचरे को नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर फेंकने के लिये जब कम-से-कम तीस ट्रैक्टरों, उनके लिये डीजल और डेढ़ सौ कर्मचारियों की न्यूनतम जरूरत का हिसाब लगा।
देश में लगभग हर जगह सीवर के पाइप और गली मुहल्लों की नालियाँ पालीथिन की थैलियों से अट गई हैं। हर कस्बे में नई सीवर लाइनों की माँग हो रही है। देश का हर छोटा बड़ा कस्बा गन्दगी और कचरे के प्रबन्धन और गन्दे पानी की निकासी के काम के लिये फौरी तौर पर बीस-बीस करोड़ रुपए माँग रहा है। पूरे देश को एक नजर में देख सकने में सक्षम प्रबन्धन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हर साल कितनी बार दोहरा देते हैं कि आधारभूत ढाँचा खड़ा करने के लिये एक मुश्त पचास लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। उसके रखरखाव के खर्चों का तो अभी हिसाब ही नहीं लगा। आज ऐसे कस्बों की संख्या लगभग तीन हजार है। इनसे छोटे उपनगरीय इलाकों की संख्या पाँच हजार को पार कर रही है। यानी जानकारों को अच्छी तरह पता था कि साफ-सफाई का काम खर्चे के लिहाज से कितना बड़ा है। जिन मौजूदा लोगों ने इस काम को जागरुकता के सहारे निपटाने की बात सोची हो उन्हें एक बार सार्वजनिक रूप से सामने बैठाकर क्या यह नही पूछा जाना चाहिए कि बगैर संसाधनों के इस लक्ष्य को हासिल करना सम्भव है भी या नहीं?
अभी तक की बात सिर्फ शहरी इलाके की हुई है। देश का दो तिहाई हिस्सा यानी देश का गाँव बाकी है। इधर नई सरकार ने छह लाख गाँवों में घर-घर शौचालय का नया नारा भी लगाया है। कुछ होता दिखाने के लिये और कुछ तो तय हुआ नहीं था। सिर्फ जागरुकता अभियान का ही खाका बना था। सो प्रचार अभियान इतने जोर-शोर से चला है कि भारत सरकार अब तक प्रचार के काम पर ही कोई नौ सौ करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
शौच के लिये खेत या सुबह के पहले नीम अन्धेरे या झुटपुटे में सड़क किनारे बैठने का चलन खत्म कराने के लिये गाँव में घर-घर शौचालय बनवाने का अभियान सोचा गया। सोचने वालों ने यह भी देख जरूर लिया होगा कि अभी-अभी यानी सिर्फ 68 साल पहले आजाद हुए देश के गाँव वालों की माली हालत क्या है।
अभी तक सिर्फ जरूरत का अनाज पैदा करने लायक ही हम बन पाए हैं। एड़ी से चोटी का दम लगाने के बावजूद खेती की ज़मीन में सिर्फ 50 फीसद खेतों तक सिंचाई प्रणाली का इन्तजाम कर पाये हैं। औसत गाँव में छोटे किसान और खेतिहर मज़दूर अभी कच्चे मकान और हर साल फूस के ऊपर खप्पर रखकर छत बनाने लायक ही हुए हैं।
पूरी ताकत लगाने के बावजूद हर व्यक्ति को न्यूनतम 30 ग्राम चिकनाई यानी खाने का तेल मुहैया हो जाये, गाँव के औसत किसान और मजदूर की यह सामर्थ्य ही बनते-बनते ही बन रही है। उसके लिये न्यूनतम कपड़े लत्तों का तो अभी अता-पता ही नहीं है।
उसे कमोड वाले शौचालय मुहैया हो जाने की बात जिसने भी सोची हो बड़ी अच्छी बात है लेकिन जागरुकता अभियान के सहारे यह काम हो जाएगा ऐसा सोचने वालों से आमने-सामने बैठकर बात करनी चाहिए। चलिए वाणिज्य में पटु योजनाकार देशी-विदेशी वित्तीय संस्थानों से इस काम के लिये एक लाख करोड़ का इन्तजाम भी हमें बता सकते हैं।
लेकिन क्या वे यह बता पाएँगे कि शहरों की अभी सिर्फ तीस-चालीस साल पुरानी सीवर प्रणाली और गन्दे पानी की निकासी की प्रणाली का क्या हाल हो गया है। सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों से निकले पानी को गाँव से बाहर ले जाने में क्या खर्चा बैठेगा?
देश में लगभग हर जगह सीवर के पाइप और गली मुहल्लों की नालियाँ पालीथिन की थैलियों से अट गई हैं। हर कस्बे में नई सीवर लाइनों की माँग हो रही है। देश का हर छोटा बड़ा कस्बा गन्दगी और कचरे के प्रबन्धन और गन्दे पानी की निकासी के काम के लिये फौरी तौर पर बीस-बीस करोड़ रुपए माँग रहा है। पूरे देश को एक नजर में देख सकने में सक्षम प्रबन्धन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हर साल कितनी बार दोहरा देते हैं कि आधारभूत ढाँचा खड़ा करने के लिये एक मुश्त पचास लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। उसके रखरखाव के खर्चों का तो अभी हिसाब ही नहीं लगा।
 ऐसे सोच-विचार और हिसाब-किताब और योजना बनाने का काम पिछले साल तक योजना आयोग किया करता था। लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। या अब उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग क्या करेगा यह साफतौर पर अभी पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से तरह-तरह के अभियान या नारे चालू हुए हैं उनके क्रियान्वयन के लिये इस नीति आयोग को कम-से-कम खाका बनाकर तो देना ही पड़ेगा।
ऐसे सोच-विचार और हिसाब-किताब और योजना बनाने का काम पिछले साल तक योजना आयोग किया करता था। लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। या अब उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग क्या करेगा यह साफतौर पर अभी पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से तरह-तरह के अभियान या नारे चालू हुए हैं उनके क्रियान्वयन के लिये इस नीति आयोग को कम-से-कम खाका बनाकर तो देना ही पड़ेगा। साथ ही उसे यह भी बताते चलना पड़ेगा कि इन अभियानों या कार्यक्रमों पर खर्चा क्या बैठेगा। और तभी पता चलेगा कि अगर नापतोल करने लायक स्वच्छता अभियान का कोई लक्ष्य बना है तो उस पर कुल खर्चा क्या आएगा। और अगर बगैर नापतोल वाला कोई लक्ष्य बना है और सिर्फ जागरुकता ही हमारा मकसद है तो फिर कोई बात नहीं। तब तो यह बहुत ही सुन्दर सदइच्छा है जिसकी आलोचना समालोचना की कोई गुंजाईश ही नहीं है।
फिर भी इस मामले में हमें समय निकालकर कभी पिछली सरकार के स्वच्छता मिशन पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। क्योंकि प्रचार-प्रसार में कच्ची पिछली सरकार के इस मिशन के बारे में ज्यादा पता नहीं चला था। आजादी के बाद से अब तक क्या होता आया है? कितना हुआ है? जो कुछ नहीं हो पाया उसमें क्या-क्या अड़चनें आईं? जो कुछ हो रहा था वह किस स्थिति में था और उसमें नया क्या जोड़ने की जरूरत है? या उसे जारी रखने की कितनी ज्यादा जरूरत है?
 ये सब ऐसी बाते हैं जिन्हें देखते चलने से ही हम मौजूदा चुनौतियों से पार पा सकते हैं। और फिर देश के पैमाने पर साफ-सफाई का काम रंग रोगन या पुताई का काम नहीं है बल्कि यह काम देश के स्वास्थ्य और देश की सकल उत्पादकता से जुड़ा मामला है। कम-से-कम ऐसे मामले में ज्यादा सयानपन दिखाना ठीक नहीं होगा। सिर्फ साफ-सफाई ही जब इतनी बड़ी चुनौती दिख रही हो तो स्मार्ट सिटी के नारे पर यह टिप्पणी की जा सकती है कि कहीं ये सिटी ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में न फँस जाएँ।
ये सब ऐसी बाते हैं जिन्हें देखते चलने से ही हम मौजूदा चुनौतियों से पार पा सकते हैं। और फिर देश के पैमाने पर साफ-सफाई का काम रंग रोगन या पुताई का काम नहीं है बल्कि यह काम देश के स्वास्थ्य और देश की सकल उत्पादकता से जुड़ा मामला है। कम-से-कम ऐसे मामले में ज्यादा सयानपन दिखाना ठीक नहीं होगा। सिर्फ साफ-सफाई ही जब इतनी बड़ी चुनौती दिख रही हो तो स्मार्ट सिटी के नारे पर यह टिप्पणी की जा सकती है कि कहीं ये सिटी ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में न फँस जाएँ।